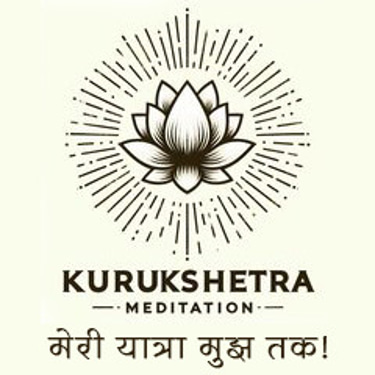आदि गुरू शंकराचार्य
अद्वैतवाद
SAINTS
10/28/20241 मिनट पढ़ें
आदि शंकराचार्य
आदि शंकराचार्य भारत के महान संत, विद्वान और दार्शनिक रहे है। उनका जन्म लगभग 788 ईस्वी में केरल के कालड़ी नामक स्थान पर हुआ। वे वेदांत के अद्वैत (अद्वैतवाद) सिद्धांत के महान प्रवर्तक माने जाते हैं और हिंदू धर्म में सुधार और पुनरुद्धार के लिए जाने जाते हैं।
शंकराचार्य का जीवन धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में सुधार के लिए समर्पित रहा । बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। आठ वर्ष की आयु में उन्होंने वेदों का अध्ययन पूरा कर लिया था और उन्होंने सन्यास लेने का निर्णय लिया। गुरु गोविन्दपाद, जिन्होंने उन्हें अद्वैत वेदांत का ज्ञान दिया।
मुख्य शिक्षाएँ और सिद्धांत
आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की शिक्षा दी, जिसका मूल सिद्धांत है कि "ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः" अर्थात ब्रह्म (ईश्वर) ही सत्य है और यह संसार एक माया है। जीवात्मा और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है; वे दोनों एक ही हैं। उनके अनुसार, आत्मा और परमात्मा का भेद केवल अज्ञान का परिणाम है और ज्ञान द्वारा इस अज्ञान को दूर कर आत्म-साक्षात्कार किया जा सकता है।
प्रमुख कार्य
शंकराचार्य ने वेदांत की शिक्षा को पूरे भारत में फैलाने के लिए चार मठ (मठ) स्थापित किए, जो कि आज भी प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र माने जाते हैं:
1. शृंगेरी मठ (कर्नाटक) - दक्षिण भारत के लिए
2. ज्योतिष मठ (उत्तराखंड) - उत्तर भारत के लिए
3. द्वारका मठ (गुजरात) - पश्चिम भारत के लिए
4. पुरी मठ (ओडिशा) - पूर्वी भारत के लिए
उन्होंने "प्रस्थानत्रयी" (ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और उपनिषद) पर महत्वपूर्ण भाष्य (टिप्पणी) लिखे, जो अद्वैत वेदांत के विचारों को स्पष्ट करते हैं और आज भी हिन्दू धर्म के दार्शनिक पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा माने जाते हैं।
आदि शंकराचार्य ने भारत के चार कोनों में चार प्रमुख मठों (पीठों) की स्थापना की थी। इन मठों का उद्देश्य हिन्दू धर्म के अद्वैत वेदांत सिद्धांत को संरक्षित और प्रचारित करना था। चार मठों की स्थापना के पीछे शंकराचार्य का उद्देश्य पूरे देश में वेदांत की शिक्षा को एकसमान फैलाना था, जिससे भारतीय समाज में धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना का संचार हो सके। इन मठों का संचालन अद्वैत वेदांत की परंपरा में होता है, और इनके प्रमुख को शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है।
यहाँ चार मठों का संक्षिप्त विवरण है:
1. शृंगेरी शारदा पीठ (दक्षिण मठ)
- स्थान: शृंगेरी, कर्नाटक
- स्थापना: लगभग 8वीं शताब्दी में
- मुख्य देवता: देवी शारदा
- वेद: यजुर्वेद
- विचारधारा: अद्वैत वेदांत
- महत्व: यह मठ अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों के प्रचार और प्रसार के लिए जाना जाता है। शृंगेरी का यह मठ अद्वैत वेदांत के अध्ययन का प्रमुख केंद्र है और दक्षिण भारत के लोगों के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा का स्रोत है। यहां से अद्वैत वेदांत के विद्वानों और साधुओं को दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाता है।
- विशेष घटना: शंकराचार्य ने यहाँ एक मेंढक और सांप को एक साथ धूप से बचने के लिए बैठे देखा, और यह देखकर उन्होंने इसे शांति और ज्ञान का स्थल माना। इसलिए उन्होंने यहाँ मठ की स्थापना की।
2. ज्योतिर्मठ (उत्तर मठ)
- स्थान: बद्रीनाथ, उत्तराखंड
- स्थापना: 8वीं शताब्दी
- मुख्य देवता: भगवान नारायण
- वेद: अथर्ववेद
- विचारधारा: अद्वैत वेदांत
- महत्व: यह मठ उत्तर भारत में अद्वैत वेदांत का प्रमुख केंद्र है और हिमालय क्षेत्र के साधु-संतों के लिए मुख्य स्थल है। यहाँ के शंकराचार्य बद्रीनाथ मंदिर के पूजापाठ में विशेष योगदान देते हैं। यह मठ हिमालय क्षेत्र के हिंदू धर्म और संस्कृतियों को एकसूत्र में पिरोने का कार्य करता है।
- विशेषता: ज्योतिर्मठ से हिंदू धर्म के साधना, तपस्या, और वेदांत के अध्ययन के प्रति गहरी निष्ठा बनी रहती है, जो हिमालय की शांति और आध्यात्मिकता से प्रेरित है।
3. द्वारका शारदा पीठ (पश्चिम मठ)
- स्थान: द्वारका, गुजरात
- स्थापना: 8वीं शताब्दी
- मुख्य देवता: भगवान कृष्ण
- वेद: सामवेद
- विचारधारा: अद्वैत वेदांत
- महत्व: यह मठ पश्चिम भारत में वेदांत शिक्षा का प्रचार करता है और पश्चिमी भारत के लोगों के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। द्वारका मठ का उद्देश्य क्षेत्र में धार्मिक परंपराओं का प्रसार करना और संस्कृति का संरक्षण करना है। यहाँ के शंकराचार्य द्वारका के पौराणिक महत्व को ध्यान में रखते हुए कृष्ण भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं।
- विशेषता: इस मठ का स्थान भगवान कृष्ण की पौराणिक नगरी द्वारका में है, जिससे यह हिंदू धर्म के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विशेष महत्व रखता है।
4. गोवर्धन मठ (पूर्व मठ)
- स्थान: पुरी, ओडिशा
- स्थापना: 8वीं शताब्दी
- मुख्य देवता: भगवान जगन्नाथ
- वेद: ऋग्वेद
- विचारधारा: अद्वैत वेदांत
- महत्व: गोवर्धन मठ पूर्वी भारत के लोगों के लिए अद्वैत वेदांत का प्रमुख केंद्र है। यह मठ जगन्नाथ मंदिर के धार्मिक कार्यों और व्यवस्थाओं में सहयोग करता है। यहाँ का शंकराचार्य पुरी के धार्मिक रीति-रिवाजों को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मठ के साधु-संन्यासी पूर्वी भारत में वेदांत का प्रचार करते हैं।
- विशेषता: पुरी मठ में हर साल रथ यात्रा का आयोजन होता है, जो इस मठ के धार्मिक महत्व को दर्शाता है। यह मठ भगवान जगन्नाथ के प्रति समर्पण का प्रतीक है और भारत के प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है।
मठों की अद्वैत परंपरा में भूमिका
आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित ये चार मठ भारतीय सांस्कृतिक, धार्मिक और दार्शनिक चेतना का केंद्र बने हुए हैं। प्रत्येक मठ वेदों में से एक वेद का अध्ययन, प्रचार और संरक्षण करता है, ताकि भारत में वेदों की समृद्ध परंपरा को संरक्षित रखा जा सके। शंकराचार्य के ये चार मठ आज भी अपने-अपने क्षेत्र में हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखते हैं और वेदांत की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं।
इन मठों का एक और महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वे धर्म और समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए सन्यासियों को शिक्षा देते हैं और उन्हें समाज की सेवा में नियुक्त करते हैं।
धार्मिक सुधार
शंकराचार्य ने हिन्दू समाज में प्रचलित अंधविश्वास और कर्मकांडों का विरोध किया और लोगों को आत्मज्ञान तथा भक्ति की ओर प्रेरित किया। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिवाद और संकीर्णता को समाप्त करने का भी प्रयास किया। वे मानते थे कि केवल सत्य, ज्ञान और साधना के द्वारा ही मनुष्य आत्म-साक्षात्कार कर सकता है।
आदि शंकराचार्य के जीवन में कई ऐसी कहानियाँ और घटनाएँ हैं, जो उनके अद्वितीय ज्ञान, बुद्धिमत्ता और अद्वैत सिद्धांत की गहराई को दर्शाती हैं। यहां कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं:
1. माँ के अंतिम संस्कार की कहानी
आदि शंकराचार्य के सन्यास लेने के बाद, उनकी माँ की इच्छा थी कि शंकराचार्य उनकी मृत्यु के समय उनके पास रहें। माँ के प्रति अपने प्रेम और कर्तव्य का सम्मान करते हुए, शंकराचार्य उनकी अंतिम घड़ी में उनके पास पहुँचे। परंतु, सन्यासियों को अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए गाँव वालों ने उनका साथ नहीं दिया। शंकराचार्य ने माँ का अंतिम संस्कार खुद ही किया, और यह दर्शाया कि सन्यास और परिवार के प्रति कर्तव्य में कोई विरोधाभास नहीं है। यह घटना उनके करुणा और त्याग के गुणों को दर्शाती है।
2. मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ
शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ (विचार-विमर्श) भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। मंडन मिश्र, जो एक अत्यंत विद्वान और धार्मिक व्यक्ति थे, अपने समय के सर्वश्रेष्ठ न्यायविद् माने जाते थे। शंकराचार्य ने उन्हें अद्वैत सिद्धांत का ज्ञान देने के लिए शास्त्रार्थ का प्रस्ताव रखा। यह शास्त्रार्थ कई दिनों तक चला। अंततः, मंडन मिश्र पराजित हुए और शंकराचार्य के शिष्य बन गए। यह घटना शंकराचार्य के ज्ञान और तर्क की अद्वितीयता को दिखाती है।
3. कामासुत्र का अनुभव
मंडन मिश्र की पत्नी उभया भारती ने शंकराचार्य से पूछा कि क्या वे सभी सांसारिक अनुभवों को समझ सकते हैं, जिसमें कामासुत्र भी शामिल है। शंकराचार्य, जो सन्यासी थे, ने इसका अध्ययन नहीं किया था। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, शंकराचार्य ने कुछ समय के लिए एक राजा का शरीर धारण किया और राजा के रूप में सांसारिक अनुभवों का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद वे उभया भारती के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हुए। यह घटना दर्शाती है कि शंकराचार्य केवल शास्त्रों के ज्ञाता ही नहीं थे, बल्कि हर क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने की उनकी उत्सुकता थी।
4. काशी में चांडाल के रूप में भगवान शिव से भेंट
कहते हैं कि काशी में गंगा स्नान के बाद शंकराचार्य रास्ते में एक चांडाल (अस्पृश्य) से मिले, जो उनके मार्ग में खड़ा था। शंकराचार्य ने उसे हटने के लिए कहा, परंतु उस चांडाल ने उत्तर दिया कि यदि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, तो यह भेदभाव क्यों? उस चांडाल में भगवान शिव का रूप था और वे शंकराचार्य को अद्वैत का वास्तविक ज्ञान देने के लिए प्रकट हुए थे। इस घटना ने शंकराचार्य को यह समझाया कि सच्चा अद्वैत वही है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता।
5. मगरमच्छ और सन्यास ग्रहण की कहानी
कहते हैं कि एक बार जब शंकराचार्य गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, तो एक मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। यह देखकर उनकी माँ घबरा गईं। शंकराचार्य ने अपनी माँ से अनुमति माँगी कि वे सन्यास ग्रहण कर सकें ताकि वे मुक्त हो सकें। माँ ने सहमति दी, और मगरमच्छ ने शंकराचार्य को छोड़ दिया। इस घटना के माध्यम से शंकराचार्य ने संन्यास के प्रति अपनी अटूट निष्ठा दिखाई और उसी क्षण से उन्होंने सन्यासी जीवन अपना लिया।
6. कपालिक योगी की परीक्षा
शंकराचार्य की प्रसिद्धि के कारण एक कपालिक योगी उनके पास आया और उनसे प्रार्थना की कि वे उनकी पूजा के लिए अपना शरीर अर्पित करें। शंकराचार्य तैयार हो गए, लेकिन उनके शिष्य पद्मपाद ने कपालिक की योजना का खुलासा किया और शंकराचार्य को बचाया। यह घटना दर्शाती है कि शंकराचार्य ने अपने जीवन का बलिदान करने में भी कोई संकोच नहीं किया और उन्होंने सच्चे ज्ञान के लिए अपने शरीर तक का त्याग करने की तैयारी दिखाई।
7. शृंगेरी मठ की स्थापना
शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना की थी। जब वे शृंगेरी पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक सांप मेंढ़क को मारने की बजाय उसे धूप से बचाने के लिए अपने फन से ढक कर खड़ा था। इस दृष्य को देखकर उन्होंने वहाँ मठ स्थापित किया, जो आज भी ज्ञान और शांति का प्रतीक है।
इन कहानियों के माध्यम से आदि शंकराचार्य का व्यक्तित्व केवल एक दार्शनिक ही नहीं, बल्कि एक साहसी और समर्पित आध्यात्मिक नेता के रूप में भी सामने आता है, जिन्होंने जीवन में सेवा, निष्ठा, और करुणा का मार्ग अपनाया।
आदि शंकराचार्य की धार्मिक शिक्षाएँ अद्वैत वेदांत पर आधारित हैं और हिंदू धर्म में आत्मा और ब्रह्म के एकत्व पर जोर देती हैं। शंकराचार्य ने भारतीय दार्शनिक परंपरा में एक गहरा प्रभाव छोड़ा, जिसमें उन्होंने ज्ञान और भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। उनके विचारों ने हिंदू धर्म में दार्शनिक सोच को एक नया आयाम दिया।
यहाँ आदि शंकराचार्य की प्रमुख धार्मिक शिक्षाएँ दी गई हैं:
1. अद्वैत वेदांत का सिद्धांत
- शंकराचार्य की सबसे प्रमुख शिक्षा अद्वैत वेदांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है "गैर-द्वैत" या "अद्वैत"। उनके अनुसार, ब्रह्म और आत्मा (जीव) एक ही हैं, और दोनों में कोई भेद नहीं है। ब्रह्म (परमात्मा) ही एकमात्र वास्तविकता है, और सारा जगत उसी का प्रतिबिंब है।
- अद्वैत वेदांत के अनुसार, संसार मिथ्या (भ्रम) है और ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। माया के कारण हमें संसार और आत्मा में भेद दिखता है, परंतु वास्तविकता में आत्मा और परमात्मा एक ही हैं।
2. माया का सिद्धांत
- शंकराचार्य ने माया (भ्रम) के सिद्धांत पर बल दिया। उनके अनुसार, माया ही वह शक्ति है, जो आत्मा को परमात्मा से अलग दिखाती है और संसार का भ्रम उत्पन्न करती है। माया के कारण ही व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचान नहीं पाता।
- माया से उत्पन्न इस भौतिक जगत को उन्होंने असत्य और परिवर्तनशील माना। माया के प्रभाव से मुक्ति ही आत्मा के परमात्मा में विलीन होने का मार्ग है।
3. ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से मोक्ष
- शंकराचार्य के अनुसार, मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र मार्ग ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति स्वयं को माया से मुक्त कर ब्रह्म को पहचान लेता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मज्ञान के माध्यम से ही आत्मा की मुक्ति संभव है।
- उनका मानना था कि कर्मकांड और धार्मिक अनुष्ठानों से अधिक महत्व ज्ञान का है। आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान से व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकता है और जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है।
4. निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म का सिद्धांत
- शंकराचार्य ने ब्रह्म को दो रूपों में समझाया: निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म का अर्थ है कि ब्रह्म निर्गुण, निराकार, और असीम है, जबकि सगुण ब्रह्म का अर्थ है कि ईश्वर को नाम, रूप और गुण के साथ देखा जा सकता है।
- उन्होंने समझाया कि निर्गुण ब्रह्म ही परम सत्य है, और सगुण ब्रह्म को पूजा-उपासना के माध्यम से समझा जा सकता है। यह उपासना का मार्ग भक्तों के लिए है, जबकि ज्ञान के साधक निर्गुण ब्रह्म की साधना करते हैं।
5. अहंकार का त्याग
- शंकराचार्य ने अहंकार को आत्मज्ञान में सबसे बड़ी बाधा माना। उन्होंने कहा कि जब तक व्यक्ति का अहंकार जीवित है, तब तक वह आत्मा और परमात्मा के एकत्व को नहीं समझ सकता।
- उनके अनुसार, मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अहंकार का त्याग करना होगा और अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना होगा। यह आत्म-समर्पण और अहंकार का विलय ही ईश्वर को पाने का मार्ग है।
6. व्यक्ति का आत्मा ही ईश्वर है
- शंकराचार्य ने कहा कि हर व्यक्ति का आत्मा ही परमात्मा का अंश है और सभी में ब्रह्म का वास है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर की खोज बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर करनी चाहिए।
- उन्होंने यह भी कहा कि आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है, और मृत्यु केवल शरीर का नाश है, आत्मा का नहीं। आत्मा का सच्चा स्वरूप जानने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर झांकना चाहिए।
7. ज्ञान और भक्ति का संतुलन
- शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग को मोक्ष प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग माना, लेकिन उन्होंने भक्ति का भी समर्थन किया। उनके अनुसार, ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, और दोनों ही मार्ग व्यक्ति को ईश्वर के समीप ले जाते हैं।
- उन्होंने उपदेश दिया कि भक्तों के लिए सगुण ब्रह्म की भक्ति, प्रेम, और पूजा आवश्यक है, जबकि ज्ञानी लोग ब्रह्म के निराकार रूप का ध्यान कर सकते हैं।
8. धर्म का सही अर्थ
- शंकराचार्य के अनुसार, धर्म का उद्देश्य व्यक्ति को सत्य की ओर ले जाना है। उन्होंने धर्म के बाहरी कर्मकांडों की अपेक्षा आत्मज्ञान, भक्ति और सत्य पर आधारित धर्म का समर्थन किया।
- उनका मानना था कि धर्म का अनुसरण करते समय व्यक्ति को अहंकार, द्वेष और भेदभाव का त्याग करना चाहिए और सभी को ईश्वर का अंश मानना चाहिए।
9. कर्म का महत्व
- यद्यपि शंकराचार्य ने ज्ञान को मोक्ष का मुख्य मार्ग माना, लेकिन उन्होंने कर्म का भी महत्व बताया। उनके अनुसार, सांसारिक कर्तव्यों को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान के साथ किया जाना चाहिए।
- कर्म को ईश्वर को अर्पण करते हुए निष्काम भाव से करना चाहिए, जिससे व्यक्ति पर कर्मों का कोई बंधन नहीं रहता और वह ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है।
10. गुरु का महत्व
- शंकराचार्य ने गुरु को आत्मज्ञान प्राप्त करने में महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार, आत्मज्ञान की जटिलताओं को समझने के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है, जो शिष्य का मार्गदर्शन करता है और उसे सत्य का बोध कराता है।
- उन्होंने गुरु को ईश्वर का प्रतिनिधि माना और कहा कि गुरु ही वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति को ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है।
आदि शंकराचार्य की शिक्षाएँ हिंदू धर्म और दर्शन में मौलिक भूमिका निभाती हैं और व्यक्ति को आत्मज्ञान, भक्ति, और मोक्ष के मार्ग पर प्रेरित करती हैं। उनकी अद्वैत वेदांत शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, और यह भौतिक संसार केवल माया का भ्रम है।
मृत्यु
आदि शंकराचार्य का जीवन अल्पकालिक था, और मात्र 32 वर्ष की आयु में, 820 ईस्वी में केदारनाथ के पास उनकी मृत्यु हो गई। उनके कार्यों और शिक्षाओं ने हिन्दू धर्म को एक नई दिशा दी और भारत के आध्यात्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
शंकराचार्य की शिक्षाएँ आज भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और उनका योगदान भारतीय समाज में अमिट है। उनके जीवन की कहानी हमें ज्ञान, समर्पण और भक्ति का महत्व सिखाती है।
यह सामग्री इंटरनेट के माध्यम से तैयार की गयी है, ज्यादा जानकारी के लिए, उपरोक्त से संबन्धित संस्थान से सम्पर्क करें ।
उपरोक्त सामग्री व्यक्ति विशेष को जानकारी देने के लिए है, किसी समुदाय, धर्म, संप्रदाय की भावनाओं को ठेस या धूमिल करने के लिए नहीं है ।
हमारा उद्देश्य केवल सजगता बढ़ाना है ,हम जन साधारण को संतो, ध्यान विधियों ,ध्यान साधना से संबन्धित पुस्तकों के बारे मे जानकारी , इंटरनेट पर मौजूद सामग्री से जुटाते है । हम किसी धर्म ,संप्रदाय ,जाति , कुल ,या व्यक्ति विशेष की मान मर्यादा को ठेस नही पहुंचाते है । फिर भी जाने अनजाने , यदि किसी को कुछ सामग्री सही प्रतीत नही होती है , कृपया हमें सूचित करें । हम उस जानकारी को हटा देंगे ।
website पर संतो ,ध्यान विधियों , पुस्तकों के बारे मे केवल जानकारी दी गई है , यदि साधकों /पाठकों को ज्यादा जानना है ,तब संबन्धित संस्था ,संस्थान या किताब के लेखक से सम्पर्क करे ।
© 2024. All rights reserved.