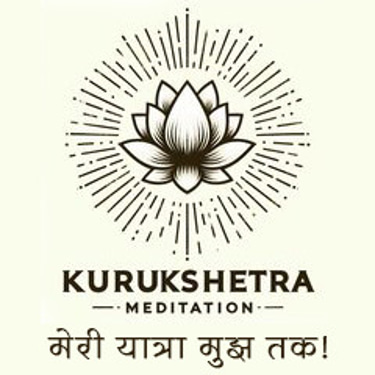बृहदारण्यक उपनिषद
Blog post description.
BLOG
12/14/20241 मिनट पढ़ें
बृहदारण्यक उपनिषद
बृहदारण्यक उपनिषद वेदों के प्रमुख उपनिषदों में से एक है और यह यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। यह उपनिषद प्राचीन भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है और इसमें आत्मा, ब्रह्म, जीवन, मृत्यु, और ब्रह्मा के साथ एकत्व की अवधारणाएँ प्रस्तुत की गई हैं। बृहदारण्यक उपनिषद का संवाद और दर्शन गहरे आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों से भरा हुआ है।
बृहदारण्यक उपनिषद का संक्षिप्त परिचय
यह उपनिषद मुख्य रूप से एक संवादात्मक रूप में है, जिसमें विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों के बीच गहरे धार्मिक और दार्शनिक वार्तालाप होते हैं। इस उपनिषद में चर्चा के मुख्य विषय आत्मा, ब्रह्म, संसार की उत्पत्ति, सृष्टि का उद्देश्य और जीवन के अंतर्गत शाश्वत सत्य के हैं।
बृहदारण्यक उपनिषद की संरचना
बृहदारण्यक उपनिषद चार प्रमुख खंडों (प्रकाश, अन्वक्षिका, शांति, उपनिषद) में बांटा गया है और इसमें कुल सात "ब्राह्मण" हैं। इसके भीतर अन्य लघु उपनिषदों, सूत्रों और कथाओं का भी समावेश है, जो दर्शन और तात्त्विक विचारों को समृद्ध करते हैं।
मुख्य विषय और गहरे विचार
1. ब्रह्म और आत्मा का एकत्व
बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरा विचार है कि आत्मा और ब्रह्म का कोई भेद नहीं है। उपनिषद में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्रह्म (परम सत्य) ही आत्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। यह अद्वैत (Non-dualism) की अवधारणा को पुष्ट करता है कि जो ब्रह्म है, वही आत्मा है, और इसी सच्चाई का बोध ही व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है।
2. "अहं ब्रह्मास्मि" (मैं ब्रह्म हूँ)
बृहदारण्यक उपनिषद में इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है कि व्यक्ति स्वयं ब्रह्म का ही अंश है। इसे समझाते हुए कहा जाता है, "अहं ब्रह्मास्मि", अर्थात् "मैं ब्रह्म हूँ।" इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। आत्मा ब्रह्म का ही रूप है, और इस अद्वैत सत्य को जानना ही सर्वोत्तम ज्ञान है।
3. "तत् त्वम् असि" (तुम वही हो)
यह वाक्य बृहदारण्यक उपनिषद में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका अर्थ है कि तुम वही हो, जो ब्रह्म है। यह एक गहरी और महत्वपूर्ण शिक्षा है, जो यह बताती है कि ब्रह्म और आत्मा का कोई भेद नहीं है। जब व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, तो वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है और वह ब्रह्म से एक हो जाता है।
4. जीवन और मृत्यु का रहस्य
बृहदारण्यक उपनिषद में जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर भी गहरे विचार प्रस्तुत किए गए हैं। यह उपनिषद यह सिखाता है कि आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है; यह शाश्वत है। जब शरीर मरता है, तो आत्मा नष्ट नहीं होती, बल्कि वह अन्य शरीर में प्रवेश करती है। जीवन और मृत्यु के पार की वास्तविकता को समझने के लिए व्यक्ति को आत्मा के सत्य का बोध होना चाहिए।
5. आत्मा का रूप और उसका अनुभव
उपनिषद में यह भी कहा गया है कि आत्मा न तो शरीर के साथ जुड़ी होती है, न वह किसी बाहरी वस्तु से प्रभावित होती है। आत्मा का असली रूप ब्रह्म है, और जब व्यक्ति ब्रह्म को अनुभव करता है, तो वह आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत के सत्य को समझ लेता है। इसका अनुभव ही शांति और मुक्तिके मार्ग पर चलता है।
6. ज्ञान का मार्ग
ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपनिषद यह बताता है कि केवल बाहरी संसार का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई में जाकर आत्म-साक्षात्कार करना चाहिए। यह उपनिषद निष्ठा (faith), ध्यान (meditation) और ज्ञान (knowledge) को आत्मा के सत्य को जानने के मुख्य मार्ग के रूप में प्रस्तुत करता है। शिष्य को गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद, उसे आत्मा के भीतर गहरे विचार करना होता है।
7. सृष्टि की उत्पत्ति
बृहदारण्यक उपनिषद में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में भी गहरी चर्चा की गई है। उपनिषद में यह बताया गया है कि ब्रह्म से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। पहले केवल ब्रह्म था, जो निराकार और निराकार था। फिर उसने अपनी इच्छाशक्ति से सृष्टि का निर्माण किया। इस सृष्टि में हर प्राणी, हर तत्व ब्रह्म का ही अंश है। सृष्टि के हर रूप में ब्रह्म का स्वरूप विद्यमान है, और यह जीवन का परम सत्य है।
8. "पुर्णमाद: पूर्णमिदं" (पूरण की अवधारणा)
यह एक महत्वपूर्ण विचार है जो उपनिषद में आता है। "पूर्णमाद: पूर्णमिदं" का अर्थ है "यह पूर्ण है, वह भी पूर्ण है।" इसका तात्पर्य है कि ब्रह्म शाश्वत और पूर्ण है, और संसार भी ब्रह्म का ही एक रूप है। जब हम ब्रह्म को समझते हैं, तो हम संसार के हर रूप को भी ब्रह्म का ही अंश मानने लगते हैं। इस विचार से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म और संसार का कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही परम सत्य का रूप हैं।
बृहदारण्यक उपनिषद का महत्व
बृहदारण्यक उपनिषद का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसमें जीवन, मृत्यु, ब्रह्म और आत्मा के अद्वैत रूप को समझाया गया है। यह उपनिषद आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मा का सत्य जानने के लिए एक गहरी और विस्तृत मार्गदर्शिका प्रस्तुत करता है। इस उपनिषद में एक ओर महत्वपूर्ण तत्व है प्रश्नोत्तरी (question-answer format) और वार्तालाप की प्रक्रिया, जो शिष्य और गुरु के बीच होती है। यह उपनिषद एक जीवनमुक्ति के मार्ग को प्रस्तुत करता है, जो संसार के भ्रम और दुख से मुक्त होने के लिए है।
बृहदारण्यक उपनिषद के गहरे विचार भारतीय तात्त्विक दर्शन का आधार हैं, और इसमें आत्मा, ब्रह्म, जीवन और मृत्यु के बारे में गहरी शिक्षाएँ दी गई हैं। इस उपनिषद का मुख्य उद्देश्य है जीवन के अद्वितीय सत्य को जानना और आत्म-ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करना। आइए हम इस उपनिषद के कुछ गहरे विचारों को विस्तार से समझें:
1. "अहं ब्रह्मास्मि" (मैं ब्रह्म हूँ)
"अहं ब्रह्मास्मि" का अर्थ है "मैं ब्रह्म हूँ", यानी आत्मा और ब्रह्म का कोई भेद नहीं है। यह एक प्रमुख सिद्धांत है, जो अद्वैत वेदांत के मूल तत्वों में से है। बृहदारण्यक उपनिषद में यह विचार बार-बार प्रस्तुत किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा (individual self) और ब्रह्म (universal consciousness) दोनों एक ही हैं। जब व्यक्ति इस सत्य को समझता है, तो वह आत्म-ज्ञान (Self-realization) प्राप्त करता है और ब्रह्म से एकत्व का अनुभव करता है।
"अहं ब्रह्मास्मि" का प्रतिपादन यह दिखाता है कि आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है, वह शाश्वत है। यह शरीर, मन और इंद्रियों से परे है। जब व्यक्ति इस अनुभव को प्राप्त करता है, तब वह स्वयं को ब्रह्म के रूप में पहचानता है और संसार की अस्थायी और भ्रमित वास्तविकता से मुक्ति प्राप्त करता है।
2. आत्मा और ब्रह्म का अद्वैत (Non-duality of Atman and Brahman)
बृहदारण्यक उपनिषद में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अद्वैत या अद्वैत वेदांत का, जो बताता है कि आत्मा और ब्रह्म का कोई भेद नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में यह भी कहा गया है कि ब्रह्म ही आत्मा का स्वरूप है। जब व्यक्ति ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता है, तो वह समझता है कि वह ब्रह्म का ही अंश है।
उपनिषद के अनुसार, ब्रह्म सर्वव्यापी है, निराकार है, और शाश्वत है। आत्मा भी उसी ब्रह्म का अंश है और वह शुद्ध चेतना है। जो व्यक्ति इस अद्वैत को समझ लेता है, वह संसार के भेदभाव से मुक्त हो जाता है और मोक्ष (Moksha) या आत्म-ज्ञान की प्राप्ति करता है।
3. जीवन और मृत्यु का रहस्य
बृहदारण्यक उपनिषद में जीवन और मृत्यु के संबंध में गहरी बातें की गई हैं। इस उपनिषद में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है। जब शरीर की मृत्यु होती है, तब आत्मा नष्ट नहीं होती, बल्कि वह शरीर छोड़कर अन्य शरीर में प्रवेश करती है। यह विचार यह दिखाता है कि आत्मा शाश्वत और अनादि है।
उपनिषद में यह भी बताया गया है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व निरंतर है। आत्मा हमेशा जीवित रहती है और वह कभी समाप्त नहीं होती। आत्मा के सत्य को जानने के बाद व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और वह शाश्वत शांति का अनुभव करता है।
4. "तत् त्वम् असि" (तुम वही हो)
बृहदारण्यक उपनिषद में "तत् त्वम् असि" का भी उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है "तुम वही हो"। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा और ब्रह्म का कोई अंतर नहीं है। यह वाक्य शिष्य को यह समझाता है कि वह जो ब्रह्म का अध्ययन कर रहा है, वह उसी ब्रह्म का अंश है।
यह विचार आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत के सिद्धांत को पुष्ट करता है। जब व्यक्ति इस सत्य को जानता है, तो वह शाश्वत ब्रह्म से एक हो जाता है, और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाता है। यह वाक्य आत्मज्ञान और आत्मसाक्षात्कार के लिए प्रेरित करता है।
5. सृष्टि का उत्पत्ति और ब्रह्म का कार्य
बृहदारण्यक उपनिषद में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में भी गहरे विचार प्रस्तुत किए गए हैं। उपनिषद में यह कहा गया है कि ब्रह्म ही सृष्टि का आधार है, और यह ब्रह्म अपनी इच्छाशक्ति से सृष्टि की रचना करता है।
पहले केवल ब्रह्म था, जो निराकार और निराकार में स्थित था। फिर ब्रह्म ने अपनी इच्छा से आत्मा का सृजन किया, और आत्मा से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ। यही ब्रह्म का कार्य है – सृष्टि का निर्माण और फिर उसका पालन और संहार। इस विचार से यह समझ में आता है कि संसार ब्रह्म का ही एक रूप है और सृष्टि के हर प्राणी में ब्रह्म का अंश है।
6. ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग
बृहदारण्यक उपनिषद में ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह मार्ग बताया गया है कि शिष्य को गुरु से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और आत्मा के सत्य का ध्यान करके उसे आत्मसात करना चाहिए। यह उपनिषद निष्ठा (faith), ध्यान (meditation) और ज्ञान (knowledge) को आत्मा के सत्य को जानने के मुख्य मार्ग के रूप में प्रस्तुत करता है।
जब व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करता है, तब वह ब्रह्म के करीब पहुँचता है। गुरु की शिक्षा और आत्मा के सत्य का अनुभव उसे ब्रह्म के साथ एकत्व की ओर ले जाता है। यही सर्वोत्तम ज्ञान है, और यही शांति और मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करता है।
7. "पूर्णमाद: पूर्णमिदं" (पूर्णता की अवधारणा)
बृहदारण्यक उपनिषद में पूर्णता या "पूर्णमाद: पूर्णमिदं" का विचार प्रस्तुत किया गया है, जिसका अर्थ है "यह पूर्ण है, वह भी पूर्ण है।" इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्म पूर्ण है और संसार भी ब्रह्म का ही रूप है। ब्रह्म और संसार का कोई भेद नहीं है।
यह विचार यह सिद्ध करता है कि ब्रह्म और सृष्टि दोनों शाश्वत और एक रूप हैं। जब व्यक्ति इस सत्य को जानता है, तो वह हर चीज में ब्रह्म का अनुभव करता है और संसार को ब्रह्म का ही अंश मानता है। यही ब्रह्म का पूर्ण रूप है, जो शांति और आंतरिक संतुलन की ओर मार्गदर्शन करता है।
बृहदारण्यक उपनिषद के गहरे विचारों को समझने से हमें यह बोध होता है कि ब्रह्म और आत्मा का कोई भेद नहीं है। जब व्यक्ति आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत को समझता है, तो वह संसार की असलियत को जानता है और ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। यह उपनिषद आत्म-ज्ञान और ब्रह्म-ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, जिससे व्यक्ति शाश्वत शांति, मुक्ति और आनंद प्राप्त करता है।
बृहदारण्यक उपनिषद एक अत्यंत महत्वपूर्ण वेदांत ग्रंथ है जो यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। इसमें विभिन्न गहरे तात्त्विक विचारों के साथ साथ कई कथाएँ और संवाद भी मिलते हैं, जो जीवन, ब्रह्म, आत्मा, मृत्यु, और संसार के अद्वितीय सत्य को समझाने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। बृहदारण्यक उपनिषद की प्रमुख कहानी याज्ञवल्क्य और उदयवल्क्य के संवाद से संबंधित है, जो इसके गहरे दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करते हैं।
कहानी का सारांश:
यह कहानी एक महत्वपूर्ण संवाद पर आधारित है जो याज्ञवल्क्य (जो एक महान ऋषि थे) और उनके शिष्य उदयवल्क्य के बीच हुआ था। यह संवाद जीवन के गहरे तात्त्विक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत किया गया है।
1. याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी का संवाद:
कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब याज्ञवल्क्य ने अपने घर से संन्यास लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा कि वह अपना धन और संपत्ति उसे दे रहे हैं, क्योंकि वह संन्यास लेने जा रहे हैं। इस पर मैत्रेयी ने उनसे पूछा कि क्या धन से अमरता प्राप्त की जा सकती है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि धन केवल भौतिक रूप से सुख और समृद्धि दे सकता है, लेकिन आत्मा का ज्ञान और ब्रह्म का बोध ही अमरता और वास्तविक स्वतंत्रता का मार्ग है।
इस संवाद में याज्ञवल्क्य ने यह स्पष्ट किया कि केवल भौतिक संपत्ति से जीवन की शाश्वत सच्चाई का अनुभव नहीं किया जा सकता। सच्चा ज्ञान आत्मा का है, जो ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार, यह संवाद एक गहरे तात्त्विक सन्देश को प्रस्तुत करता है, जिसमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा के सत्य को जानना है।
2. याज्ञवल्क्य का ज्ञान और अद्वैत का सिद्धांत:
याज्ञवल्क्य के साथ संवाद के दौरान, उन्होंने यह सिद्धांत बताया कि आत्मा और ब्रह्म का कोई भेद नहीं है, और आत्मा को जानने से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। यही गहरी शिक्षाएँ "अहं ब्रह्मास्मि" (मैं ब्रह्म हूँ) और "तत् त्वम् असि" (तुम वही हो) के सिद्धांत की ओर इशारा करती हैं। याज्ञवल्क्य ने यह भी बताया कि आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है, वह शाश्वत है।
याज्ञवल्क्य के विचारों में ब्रह्म को सर्वोच्च और सर्वव्यापी माना गया है। जब व्यक्ति आत्मा को जानता है, तो वह ब्रह्म से एक हो जाता है। यह शिक्षा दर्शाती है कि ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं।
3. याज्ञवल्क्य और उदीप्य का संवाद:
एक अन्य प्रमुख कहानी बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और उदीप्य के संवाद के रूप में आती है। उदीप्य ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या आत्मा ब्रह्म से पृथक है। याज्ञवल्क्य ने उन्हें बताया कि सृष्टि ब्रह्म से उत्पन्न हुई है, और आत्मा भी ब्रह्म का ही अंश है। वह ब्रह्म का ही रूप है और जब वह इस सत्य को जानता है, तो उसे शांति प्राप्त होती है और वह संसार से मुक्त हो जाता है।
4. ज्ञान और मुक्ति का मार्ग:
याज्ञवल्क्य ने यह भी स्पष्ट किया कि सच्चा ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान है। जब व्यक्ति आत्मा के सत्य को समझता है, तो वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। मृत्यु केवल शरीर के नष्ट होने तक सीमित है, लेकिन आत्मा शाश्वत है और कभी समाप्त नहीं होती। यह विचार इस कहानी का महत्वपूर्ण तत्व है।
इस प्रकार, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य का ज्ञान और उनकी शिक्षा से यह सिखाया गया है कि ब्रह्म और आत्मा का अद्वैत (Non-duality) ही जीवन का सत्य है, और आत्मा के सत्य को जानकर ही व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है।
5. सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्म का स्वरूप:
बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने सृष्टि की उत्पत्ति को भी एक गहरे दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि ब्रह्म से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है, और वह ही सृष्टि का पालन और संहार भी करता है।
ब्रह्म के परम स्वरूप के बारे में याज्ञवल्क्य का कहना था कि ब्रह्म निराकार, निराकार और शाश्वत है। जब ब्रह्म ने अपनी इच्छा से सृष्टि का निर्माण किया, तो इस सृष्टि के हर प्राणी और हर तत्व में ब्रह्म का अंश है। यही ब्रह्म का कार्य है - सृष्टि का निर्माण और उसका पालन।
6. स्मृति और अनंतता:
अंत में बृहदारण्यक उपनिषद में यह कहा गया है कि आत्मा अनंत और शाश्वत है, और वह कभी समाप्त नहीं होती। यह आत्मा एक साधारण प्राणी से लेकर ब्रह्म तक, सभी में व्याप्त है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं, तो हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं और शाश्वत आनंद और शांति की प्राप्ति करते हैं।
बृहदारण्यक उपनिषद की कहानी में ज्ञान, जीवन, मृत्यु, ब्रह्म, और आत्मा के अद्वैत के गहरे विचारों को प्रस्तुत किया गया है। यह उपनिषद जीवन के परम उद्देश्य को समझाता है और आत्मा और ब्रह्म के सत्य का बोध कराता है। याज्ञवल्क्य के संवादों के माध्यम से यह उपनिषद यह दर्शाता है कि वास्तविक ज्ञान आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत में है और यही जीवन की शाश्वत सच्चाई है।
हमारा उद्देश्य केवल सजगता बढ़ाना है ,हम जन साधारण को संतो, ध्यान विधियों ,ध्यान साधना से संबन्धित पुस्तकों के बारे मे जानकारी , इंटरनेट पर मौजूद सामग्री से जुटाते है । हम किसी धर्म ,संप्रदाय ,जाति , कुल ,या व्यक्ति विशेष की मान मर्यादा को ठेस नही पहुंचाते है । फिर भी जाने अनजाने , यदि किसी को कुछ सामग्री सही प्रतीत नही होती है , कृपया हमें सूचित करें । हम उस जानकारी को हटा देंगे ।
website पर संतो ,ध्यान विधियों , पुस्तकों के बारे मे केवल जानकारी दी गई है , यदि साधकों /पाठकों को ज्यादा जानना है ,तब संबन्धित संस्था ,संस्थान या किताब के लेखक से सम्पर्क करे ।
© 2024. All rights reserved.