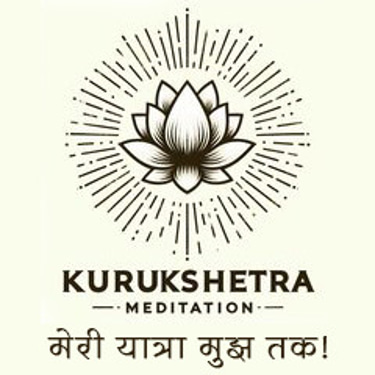गुरू नानक देव
विश्व एकता और आध्यातम
SAINTS
10/22/20241 मिनट पढ़ें
गुरु नानक देव
गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। वे एक महान संत, दार्शनिक, समाज सुधारक और कवि थे, जिन्होंने सामाजिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता और एक ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया। उनका जीवन और शिक्षाएँ सिख धर्म की आधारशिला मानी जाती हैं। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित तलवंडी नामक स्थान (अब ननकाना साहिब) में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है।
प्रारंभिक जीवन:
गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 (कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाने वाला गुरुपर्व) को हुआ था। उनके पिता का नाम कालू मेहता और माता का नाम तृप्ता देवी था। वे एक खत्री हिंदू परिवार में जन्मे थे। उनकी बहन, नानकी, गुरु नानक के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पहली व्यक्ति थीं, जिन्होंने उनकी दिव्य शक्तियों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को सबसे पहले पहचाना।
नानक बचपन से ही अद्वितीय बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक झुकाव रखते थे। वे सांसारिक चीजों की ओर आकर्षित नहीं होते थे और अक्सर ईश्वर और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर विचार करते थे। उनके अध्यात्मिक सवालों ने उन्हें अपने समय के धार्मिक रीति-रिवाजों और कुरीतियों से दूर किया।
शिक्षा और विवाह:
नानक देव की प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही उन्होंने संस्कृत, फारसी, और अन्य भाषाओं में महारत हासिल कर ली थी। उन्हें बचपन से ही धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन का गहरा शौक था। नानक का विवाह 16 साल की आयु में सुलक्खनी नामक महिला से हुआ, जो मुल्तान के पास रहने वाले मूला की बेटी थीं। उनके दो पुत्र हुए—श्रीचंद और लक्ष्मीदास। हालाँकि गुरु नानक का वैवाहिक और पारिवारिक जीवन सामान्य था, लेकिन उनका मन हमेशा आध्यात्मिकता की ओर था।
आध्यात्मिक जागरण:
गुरु नानक का आध्यात्मिक जागरण एक महत्वपूर्ण घटना थी। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने बेईं नदी के किनारे तीन दिनों तक ध्यान में लीन रहने के बाद यह घोषणा की, "न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान" (ना कोइ हिंदू, ना कोइ मुसलमान)। यह उनकी धार्मिक दृष्टि का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहाँ से उन्होंने सभी धार्मिक भेदभावों को समाप्त करने का संदेश दिया और एक ईश्वर की आराधना पर जोर दिया।
इस घटना के बाद, उन्होंने अपना शेष जीवन ईश्वर की उपासना और मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि हर व्यक्ति को एक ही ईश्वर में विश्वास करना चाहिए और सभी मनुष्यों को समानता के साथ देखना चाहिए।
गुरु नानक देव जी की आध्यात्मिक यात्रा उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जिसने सिख धर्म के सिद्धांतों और उनके जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट किया। उन्होंने चार प्रमुख "उदासियाँ" (यात्राएँ) कीं, जो उन्होंने भारत और विदेशों में ईश्वर का संदेश फैलाने के लिए कीं। इन यात्राओं में उन्होंने समाज में फैली धार्मिक कुरीतियों, अंधविश्वासों और असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया और एकेश्वरवाद, मानवता, सेवा, और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया।
गुरु नानक की आध्यात्मिक यात्रा को मुख्यतः दो भागों में बाँटा जा सकता है:
1. बचपन से लेकर आध्यात्मिक जागरण तक की यात्रा
2. चार प्रमुख उदासियाँ (धार्मिक यात्राएँ)
1. बचपन से लेकर आध्यात्मिक जागरण तक की यात्रा
प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव:
गुरु नानक बचपन से ही साधारण जीवन और सांसारिक मोह-माया से परे थे। उनका झुकाव ईश्वर, धर्म और अध्यात्म की ओर अधिक था। वे अक्सर एकांत में ध्यान में लीन रहते और संसारिक क्रियाकलापों से स्वयं को दूर रखते थे।
उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना तब घटित हुई जब वे 30 साल की उम्र में बेईं नदी के किनारे तीन दिनों तक ध्यान में डूबे रहे। इन तीन दिनों के बाद, जब वे नदी से बाहर आए, तो उन्होंने कहा, "न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान।" इस उद्घोषणा ने उनकी धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि को प्रकट किया। उन्होंने एक ऐसे धार्मिक दृष्टिकोण की नींव रखी, जिसमें कोई जात-पात, धर्म या भेदभाव नहीं था और केवल एक ईश्वर की भक्ति पर बल दिया गया।
इस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया और वे अपने शेष जीवन को एकेश्वरवाद के प्रचार और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए समर्पित कर दिया। यहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है।
2. चार प्रमुख उदासियाँ (धार्मिक यात्राएँ)
गुरु नानक देव ने अपने जीवनकाल में चार प्रमुख यात्राएँ कीं, जिन्हें उदासियाँ कहा जाता है। इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और समाजों में जाकर ईश्वर की एकता और मानवता की सेवा का संदेश देना था। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध और अन्य धर्मों के अनुयायियों से संवाद किया और उन्हें उनके धर्म के सच्चे अर्थ समझाए।
पहली उदासी (1499-1505)
भारत के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों की यात्रा:
गुरु नानक की पहली उदासी उत्तर और पूर्वी भारत में हुई। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा किया, जिनमें हरिद्वार, बनारस, पटना, गयाजी, और जगन्नाथ पुरी जैसे तीर्थ स्थल शामिल थे।
- हरिद्वार: गुरु नानक ने गंगा के तट पर देखा कि लोग सूर्य को जल चढ़ा रहे थे। उन्होंने समझाया कि यह अंधविश्वास है और ईश्वर की सच्ची पूजा मन और आत्मा से की जानी चाहिए, न कि रीति-रिवाजों के आधार पर।
- बनारस: यहाँ गुरु नानक ने पंडितों और धर्मगुरुओं के साथ संवाद किया और उन्हें ईश्वर की भक्ति और सेवा की सच्ची भावना को समझाया। उन्होंने कर्मकांड और धार्मिक दिखावे को नकारा।
दूसरी उदासी (1506-1509)
दक्षिण भारत और श्रीलंका की यात्रा:
गुरु नानक की दूसरी उदासी में उन्होंने दक्षिण भारत और श्रीलंका का दौरा किया। इस यात्रा में वे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, और श्रीलंका के विभिन्न हिस्सों में गए।
- रामेश्वरम और मदुरै: यहाँ गुरु नानक ने समाज में व्याप्त धार्मिक भेदभाव और जाति प्रथा को समाप्त करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य समान हैं और ईश्वर के सामने कोई उच्च या नीच नहीं होता।
- श्रीलंका: यहाँ उन्होंने राजा शिवनाभ से मुलाकात की और उन्हें एकेश्वरवाद और धर्म की सच्चाई के बारे में बताया। उनकी शिक्षा का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि राजा ने गुरु नानक की शिक्षाओं को आत्मसात किया।
तीसरी उदासी (1514-1517)
उत्तर पश्चिम भारत, अफगानिस्तान और फारस की यात्रा:
इस यात्रा में गुरु नानक ने अफगानिस्तान और फारस (वर्तमान ईरान) की यात्रा की। यह यात्रा महत्वपूर्ण थी क्योंकि यहाँ उन्होंने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों और सूफी संतों से संवाद किया।
- काबुल: यहाँ गुरु नानक ने सूफी संतों से मुलाकात की और उनके साथ आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की। उन्होंने सूफीवाद के तत्वों को समझा और सूफियों को भी सिखाया कि ईश्वर की सच्ची भक्ति प्रेम और मानवता की सेवा से होती है।
- मुल्तान और बगदाद: गुरु नानक ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से संवाद किया और उन्हें बताया कि सच्चा धर्म वह है जो सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का संदेश देता है। उन्होंने धार्मिकता को आडंबर और अंधविश्वास से मुक्त रखने की शिक्षा दी।
चौथी उदासी (1519-1521)
मक्का-मदीना और अरब के अन्य क्षेत्रों की यात्रा:
गुरु नानक की चौथी और सबसे महत्वपूर्ण उदासी मक्का-मदीना की यात्रा थी। इस यात्रा में उन्होंने इस्लाम के धार्मिक केंद्र मक्का-मदीना का दौरा किया और इस्लामी धर्मगुरुओं के साथ संवाद किया।
- मक्का: एक कथा के अनुसार, जब गुरु नानक मक्का पहुँचे तो उन्होंने अपने सिर को मक्का की ओर करके सोने पर कुछ मुस्लिम मौलवियों ने आपत्ति जताई। तब गुरु नानक ने कहा कि ईश्वर हर दिशा में है और किसी एक दिशा की ओर झुकाव दिखाना गलत है। इस घटना ने वहाँ के लोगों को यह समझाया कि ईश्वर सभी जगह उपस्थित है।
- मदीना और बगदाद: यहाँ गुरु नानक ने इस्लाम के विद्वानों से संवाद किया और उन्हें यह बताया कि ईश्वर की भक्ति को किसी खास रीति-रिवाज या कर्मकांड से बाँधना गलत है। उन्होंने सभी धर्मों में समानता और मानवता की सेवा का संदेश दिया।
आध्यात्मिक यात्रा का उद्देश्य और संदेश:
गुरु नानक देव जी की उदासियों का मुख्य उद्देश्य था:
1. एकेश्वरवाद का प्रचार: उन्होंने हर जगह यह संदेश दिया कि ईश्वर एक है और वह सभी धर्मों, जातियों और संस्कृतियों में समान है। किसी भी इंसान को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए।
2. मानवता की सेवा: गुरु नानक ने यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और धर्म वही है, जो मानवता की सेवा में समर्पित हो। सेवा का अर्थ केवल ईश्वर की उपासना नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों की मदद और उनके प्रति दया दिखाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
3. धार्मिक भेदभाव और अंधविश्वास का खंडन: उन्होंने हिंदू-मुस्लिम दोनों समाजों में व्याप्त अंधविश्वास और धार्मिक कुरीतियों को नकारा। वे कर्मकांडों के बजाय सत्य, ईमानदारी, और सेवा के मूल्यों को महत्व देते थे।
4. समानता और भाईचारे का संदेश: गुरु नानक ने जात-पात, धर्म, और वर्ग की सीमाओं को तोड़ने का संदेश दिया। वे मानते थे कि सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें समानता, प्रेम और करुणा के साथ एक-दूसरे के साथ रहना चाहिए।
5. सच्चा जीवन जीने की प्रेरणा: उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि उन्हें सत्य, ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन जीना चाहिए। ईश्वर की आराधना केवल मंदिरों और मस्जिदों में नहीं होती, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी ईश्वर की भक्ति की जा सकती है।
गुरु नानक की शिक्षाएँ:
गुरु नानक देव जी की शिक्षाएँ अत्यंत सरल, सजीव और मानवता पर आधारित थीं। उनकी शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य था कि मनुष्य अपने भीतर परमात्मा को पहचानें और धार्मिक भेदभाव, अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहें।
1. एक ईश्वर की उपासना (एक ओंकार):
गुरु नानक ने एक ईश्वर की भक्ति और आराधना पर जोर दिया। उनका मानना था कि ईश्वर निराकार है और वह सभी के लिए एक है। "एक ओंकार सतनाम" उनकी प्रमुख शिक्षा थी, जिसका अर्थ है कि ईश्वर एक है और वह सत्य है।
2. मानव समानता:
गुरु नानक ने जाति, धर्म, लिंग और सामाजिक भेदभाव को नकारा। उन्होंने सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखने की शिक्षा दी और कहा कि सभी लोग एक ही परमात्मा की संतान हैं।
3. नाम सिमरन (भगवान का स्मरण):
गुरु नानक ने नाम सिमरन या ईश्वर के नाम का ध्यान करने पर बल दिया। वे कहते थे कि ईश्वर का नाम जपने से आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति संसारिक मोह-माया से मुक्त हो जाता है।
4. कीरत करो (ईमानदारी से कमाओ):
गुरु नानक ने मेहनत और ईमानदारी से अपनी जीविका कमाने का महत्व बताया। उनका कहना था कि हमें दूसरों के श्रम पर निर्भर नहीं होना चाहिए और अपनी जीविका स्वयं अर्जित करनी चाहिए।
5. वंड छको (बांट कर खाओ):
गुरु नानक ने कहा कि जो कुछ भी हम कमाते हैं, उसमें से हमें ज़रूरतमंदों के साथ साझा करना चाहिए। यह मानवता की सेवा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
6. सेवा और परोपकार:
गुरु नानक ने मानवता की सेवा को धर्म का सबसे बड़ा रूप बताया। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों की निस्वार्थ सेवा में लगाई जाती है।
7. कर्म का सिद्धांत:
गुरु नानक ने कर्म के सिद्धांत को भी बहुत महत्व दिया। उनका मानना था कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है और इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए।
गुरु नानक देव जी की वाणी:
गुरु नानक देव ने अपनी शिक्षाओं को काव्य रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें "शबद" या "गुरबाणी" कहा जाता है। उनकी वाणी का संकलन सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। उनकी रचनाएँ सिख धर्म के आध्यात्मिक और धार्मिक मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में "जपजी साहिब" है, जिसे सिख धर्म के अनुयायी प्रतिदिन पढ़ते हैं।
गुरु नानक देव के जीवन से जुड़ी कहानियाँ
गुरु नानक देव जी का जीवन महानतम आध्यात्मिक और सामाजिक सुधारों से भरा हुआ था। उनके जीवन से जुड़ी कई प्रेरणादायक कहानियाँ हैं, जो उनके गहरे आध्यात्मिक ज्ञान, समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ उनके संघर्ष, और मानवता के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती हैं। ये कहानियाँ हमें जीवन में सच्चाई, न्याय, और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कहानियाँ दी जा रही हैं:
1. सज्जन ठग की कहानी
गुरु नानक जी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी सज्जन ठग की है। सज्जन नामक व्यक्ति अपने आप को धर्मात्मा और साधु के रूप में प्रस्तुत करता था, लेकिन वह यात्रियों को धोखा देकर उन्हें मारता और उनकी संपत्ति लूटता था। एक दिन गुरु नानक और उनके साथी भाई मरदाना उस इलाके से गुजरे, और सज्जन ने उन्हें भी धोखे से मारने की योजना बनाई। लेकिन गुरु नानक ने सज्जन से कहा:
"मन तो काचा, सज्जन ठगवा."
(अर्थात्: तेरा मन कच्चा है, और तू एक ठग है।)
गुरु नानक के शब्दों ने सज्जन के हृदय को छू लिया। उसने गुरु नानक के उपदेशों को सुनकर अपनी गलतियों को महसूस किया और अपने सभी पापों से पश्चाताप किया। उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बाँट दी और सच्चाई के मार्ग पर चल पड़ा। इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि सच्ची आध्यात्मिकता और सुधार तभी संभव है, जब हम अपने भीतर की बुराइयों को पहचानें और उन्हें छोड़ दें।
2. मूल मंत्र और जीवन का सत्य
गुरु नानक देव जी को जीवन के प्रारंभ से ही ईश्वर की खोज और सत्य की प्राप्ति की तीव्र इच्छा थी। वे बचपन से ही गहरे ध्यान और साधना में लीन रहते थे। एक दिन जब गुरु नानक ध्यान में लीन थे, उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने मूल मंत्र का उद्घोष किया:
"एक ओंकार सत नाम, करता पुरख, निरभउ, निरवैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद।"
इस मंत्र के माध्यम से गुरु नानक ने सिख धर्म के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। यह मंत्र हमें यह सिखाता है कि ईश्वर एक है, वह सत्य है, वह सृजनकर्ता है, और वह किसी के प्रति द्वेष या भय नहीं रखता। यह मंत्र गुरु नानक की आध्यात्मिक यात्रा का सार है।
3. दुनिया का सच्चा राजा
गुरु नानक जी का यह संदेश था कि असली राजा वह है जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। एक बार सुल्तान दौलत खान ने गुरु नानक को दरबार में बुलाया और उनके पास मौजूद धन-दौलत को दिखाया। सुल्तान ने पूछा कि उनके अनुसार सबसे बड़ा राजा कौन है। गुरु नानक जी ने उत्तर दिया कि यह सारी धन-दौलत और सत्ता तो नाशवान है, और सच्चा राजा वही है जो अपने मन और इंद्रियों को जीतता है।
गुरु नानक ने कहा:
"राजा बनना उतना मुश्किल नहीं जितना खुद को जानना और अपने अंदर के स्वार्थ, अहंकार और कामनाओं को जीतना मुश्किल है।"
इस संदेश ने सुल्तान को भी प्रभावित किया, और वह भी आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित हुआ।
4. कर्जन में गाया कीर्तन
गुरु नानक ने समाज में भक्ति के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। एक बार जब वे अपने साथियों के साथ यात्रा कर रहे थे, तो एक गाँव में पहुँचे जहाँ का जमींदार गरीब लोगों से अत्यधिक कर वसूलता था। गुरु नानक ने गाँव में जाकर कीर्तन किया और जमींदार को बुलाया। कीर्तन सुनने के बाद जमींदार को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने लोगों का कर्ज माफ कर दिया। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि आध्यात्मिकता और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन संभव है।
5. दो बर्तन में भोजन की घटना (लंगर की शुरुआत)
गुरु नानक जी के समय में समाज में जातिगत भेदभाव और ऊँच-नीच का प्रचलन था। लोग एक साथ बैठकर भोजन नहीं करते थे। गुरु नानक ने इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए लंगर की परंपरा शुरू की, जिसमें सभी लोग, चाहे किसी भी जाति, धर्म, या वर्ग के हों, एक साथ बैठकर भोजन करते थे।
एक बार गुरु नानक जी ने एक धनी व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति को दो अलग-अलग बर्तनों में भोजन करने के लिए कहा। गुरु नानक जी ने जब दोनों बर्तनों में से भोजन निकाला, तो उन्होंने धनी व्यक्ति के बर्तन से खून और गरीब व्यक्ति के बर्तन से दूध निकालते हुए कहा:
"धनी व्यक्ति का भोजन लोगों के शोषण और अन्याय से कमाया गया है, इसलिए यह खून के समान है। जबकि गरीब व्यक्ति का भोजन ईमानदारी से कमाया गया है, जो दूध के समान पवित्र है।"
यह घटना लंगर की परंपरा की नींव बनी और समाज में समानता का एक बड़ा संदेश दिया।
6. बाबर के साथ मुलाकात
जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, तो उसने कई निर्दोष लोगों को मारा और अत्याचार किए। गुरु नानक जी ने बाबर के अत्याचारों का खुलकर विरोध किया और उसे सही रास्ते पर चलने का संदेश दिया। गुरु नानक ने कहा:
"हे बाबर, तुमने निर्दोष लोगों के खून से धरती को लाल कर दिया है। यह सत्ता और धन का खेल हमेशा नहीं चलेगा। तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा।"
गुरु नानक के इस साहसिक संदेश ने बाबर को आत्मचिंतन करने के लिए मजबूर किया और उसने गुरु नानक का सम्मान किया। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि सच्चाई और साहस के सामने सबसे बड़ा शासक भी झुक सकता है।
7. नाम देव और चोर की कहानी
गुरु नानक ने अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को सचाई और ईमानदारी का महत्व बताया। एक बार उनके एक भक्त नाम देव ने किसी चोर को चोरी करते हुए देखा। नाम देव ने चोर को पहचान लिया, लेकिन उसे माफ कर दिया। बाद में जब वह चोर गुरु नानक जी के पास आया, तो गुरु नानक ने उससे कहा:
"तुम्हारी आत्मा भी जानती है कि तुमने जो किया है, वह गलत है। अब तुम्हारे पास मौका है कि तुम खुद को बदलो और सच्चे मार्ग पर चलो।"
गुरु नानक के इन शब्दों ने चोर के दिल को छू लिया, और उसने अपने सारे पापों से तौबा कर सच्चे मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।
अंतिम जीवन और निर्वाण:
गुरु नानक ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष करतारपुर (वर्तमान पाकिस्तान) में बिताए। उन्होंने 1539 ईस्वी में अपने निर्वाण से पहले अपने अनुयायियों के लिए गुरु अंगद देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु नानक की मृत्यु के बाद भी उनके संदेश और शिक्षाएँ सिख धर्म और मानवता के लिए प्रेरणास्त्रोत बनी रहीं। उनके निधन के समय हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने उनके पार्थिव शरीर पर अपने-अपने धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार करना चाहा। किंवदंती है कि जब उनके अनुयायियों ने उनके शव को उठाने के लिए चादर हटाई, तो उनके शरीर की जगह वहाँ केवल फूल मिले।
गुरु नानक देव का जीवन और उनकी शिक्षाएँ केवल सिख धर्म के अनुयायियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं। उन्होंने प्रेम, करुणा, और समानता का संदेश दिया और लोगों को एक ईश्वर की भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके जीवन का हर पहलू आध्यात्मिकता, सेवा, और सत्य की खोज का प्रतीक है, जिसे वे अपने अनुयायियों को सिखाते रहे।
सिख धर्म के दस गुरु सिख धर्म के आध्यात्मिक और सामाजिक नेतृत्व के प्रतीक हैं। ये गुरु सिखों के धार्मिक और सामाजिक सिद्धांतों की नींव रखकर सिख धर्म को विकसित और संरचित करने में मुख्य भूमिका निभाई। दसों गुरु ईश्वर के प्रति आस्था, सत्य, सेवा, समानता और न्याय के सिद्धांतों के समर्थक थे। प्रत्येक गुरु ने सिख धर्म को एक अलग दृष्टिकोण और दिशा दी, जिसने इसे एक पूर्ण धर्म के रूप में विकसित किया। यहाँ सिख धर्म के दस गुरु और उनके योगदान का वर्णन दिया गया है:
सिख धर्म के दस गुरु
1. गुरु नानक देव जी (1469-1539)
प्रथम गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे।
- मुख्य शिक्षाएँ: एकेश्वरवाद, समानता, मानवता की सेवा, और जातिवाद का विरोध।
- गुरु नानक देव ने हिंदू और मुस्लिम धर्म के भेदभाव को समाप्त किया और सभी के लिए एक ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया। उन्होंने "नाम जपो, कीरत करो, वंड छको" की शिक्षा दी, जिसका अर्थ है ईश्वर का नाम स्मरण करना, ईमानदारी से जीवन यापन करना, और जरूरतमंदों के साथ अपनी कमाई को साझा करना।
- उनकी रचनाएँ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, और उनका प्रमुख ग्रंथ "जपजी साहिब" है।
2. गुरु अंगद देव जी (1504-1552)
गुरु नानक के शिष्य भाई लहणा जी, जिन्हें गुरु अंगद देव के रूप में जाना गया।
- मुख्य योगदान: गुरु अंगद ने गुरमुखी लिपि का विकास किया, जो सिख धर्म की धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं को सहेजने के लिए महत्वपूर्ण था।
- उन्होंने गुरु नानक के विचारों को प्रचारित करने का कार्य किया और लंगर की परंपरा को मजबूत किया।
3. गुरु अमर दास जी (1479-1574)
गुरु अमर दास तीसरे गुरु थे और सिख समाज में सामाजिक सुधार के समर्थक थे।
- मुख्य योगदान: उन्होंने सिख धर्म में सत्संग और लंगर (सामूहिक भोजन) की परंपरा को प्रोत्साहित किया। उन्होंने जातिवाद और ऊँच-नीच के भेदभाव को समाप्त करने की कोशिश की।
- उन्होंने आनंद कारज (सिख विवाह समारोह) की शुरुआत की और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया, जैसे पर्दा प्रथा और सती प्रथा का विरोध।
4. गुरु राम दास जी (1534-1581)
चौथे गुरु और अमृतसर शहर के संस्थापक थे।
- मुख्य योगदान: गुरु राम दास जी ने अमृतसर शहर की नींव रखी और स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी, जो सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है।
- उन्होंने "लावां" (सिख विवाह संस्कार) की रचना की, जो आज भी सिख विवाह का मुख्य आधार है।
5. गुरु अर्जुन देव जी (1563-1606)
पाँचवे गुरु, जिन्होंने सिख धर्म को एक नई दिशा दी।
- मुख्य योगदान: उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब (आदि ग्रंथ) का संकलन किया, जिसमें सिख गुरुओं और अन्य संतों की वाणियों को संकलित किया गया।
- उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर (हरमंदिर साहिब) का निर्माण भी पूरा किया।
- गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के पहले शहीद बने, जब उन्हें मुगल शासक जहाँगीर के आदेश पर यातनाएँ दी गईं और उनकी हत्या कर दी गई।
6. गुरु हरगोबिंद जी (1595-1644)
गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र और सिखों के छठे गुरु।
- मुख्य योगदान: गुरु हरगोबिंद जी ने सिखों को आध्यात्मिकता के साथ-साथ शारीरिक और मानसिक शक्ति पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मिरी और पीरी (आध्यात्मिक और राजनैतिक शक्ति) के सिद्धांत की शुरुआत की।
- उन्होंने सिखों के लिए सैन्य प्रशिक्षण को आवश्यक बनाया और अकाल तख्त की स्थापना की, जो सिख धर्म का उच्चतम न्यायालय है।
7. गुरु हर राय जी (1630-1661)
गुरु हरगोबिंद जी के पोते, जो सिखों के सातवें गुरु बने।
- मुख्य योगदान: गुरु हर राय जी ने सैन्य शक्ति को बनाए रखा लेकिन युद्ध से बचने का मार्ग अपनाया। उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा और जड़ी-बूटियों के उपचार पर ध्यान केंद्रित किया।
- उन्होंने मानवता की सेवा के प्रति समर्पण और दया का मार्ग अपनाया और मुगल शासकों के प्रति शांतिपूर्ण रुख बनाए रखा।
8. गुरु हर कृष्ण जी (1656-1664)
गुरु हर राय जी के पुत्र और आठवें गुरु, जिन्होंने सबसे कम आयु (5 वर्ष) में गुरु की गद्दी संभाली।
- मुख्य योगदान: गुरु हर कृष्ण जी ने दिल्ली में प्लेग महामारी के दौरान रोगियों की सेवा की और उन्हें राहत दी।
- 8 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने सिखों को सेवा और परोपकार का संदेश दिया।
9. गुरु तेग बहादुर जी (1621-1675)
नौवें गुरु, जिन्हें मानव अधिकारों के संरक्षक के रूप में जाना जाता है।
- मुख्य योगदान: गुरु तेग बहादुर ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अपने प्राणों की आहुति दी। मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा हिंदुओं को जबरन इस्लाम में परिवर्तित करने का विरोध करने पर उन्हें शहीद किया गया।
- उनका शहीद होना धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए एक प्रतीक बन गया।
10. गुरु गोबिंद सिंह जी (1666-1708)
दसवें और अंतिम सिख गुरु, जिन्होंने सिख धर्म में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया।
- मुख्य योगदान: गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों का एक अनुशासित और संगठित समुदाय है। उन्होंने "पाँच ककार" (केश, कंघा, कड़ा, कच्छा, कृपाण) को खालसा सिखों के लिए अनिवार्य बनाया।
- गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का अंतिम और शाश्वत गुरु घोषित किया और इसके बाद किसी भी मानव गुरु की परंपरा को समाप्त कर दिया।
- उन्होंने मुगलों और अन्य शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ीं और सिखों को सामाजिक न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खड़े होने का मार्ग दिखाया।
सिख धर्म के दसों गुरु समाज में आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने धर्म और समाज में समानता, सेवा, न्याय और मानवता की स्थापना की। गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु घोषित करने के साथ ही सिख धर्म की गुरु परंपरा का अंत हुआ, लेकिन उनके विचार और शिक्षाएँ आज भी सिख समाज के नैतिक और धार्मिक मार्गदर्शन का स्तंभ बनी हुई हैं।
यह सामग्री इंटरनेट के माध्यम से तैयार की गयी है, ज्यादा जानकारी के लिए, उपरोक्त से संबन्धित संस्थान से सम्पर्क करें ।
उपरोक्त सामग्री व्यक्ति विशेष को जानकारी देने के लिए है, किसी समुदाय, धर्म, संप्रदाय की भावनाओं को ठेस या धूमिल करने के लिए नहीं है ।
हमारा उद्देश्य केवल सजगता बढ़ाना है ,हम जन साधारण को संतो, ध्यान विधियों ,ध्यान साधना से संबन्धित पुस्तकों के बारे मे जानकारी , इंटरनेट पर मौजूद सामग्री से जुटाते है । हम किसी धर्म ,संप्रदाय ,जाति , कुल ,या व्यक्ति विशेष की मान मर्यादा को ठेस नही पहुंचाते है । फिर भी जाने अनजाने , यदि किसी को कुछ सामग्री सही प्रतीत नही होती है , कृपया हमें सूचित करें । हम उस जानकारी को हटा देंगे ।
website पर संतो ,ध्यान विधियों , पुस्तकों के बारे मे केवल जानकारी दी गई है , यदि साधकों /पाठकों को ज्यादा जानना है ,तब संबन्धित संस्था ,संस्थान या किताब के लेखक से सम्पर्क करे ।
© 2024. All rights reserved.