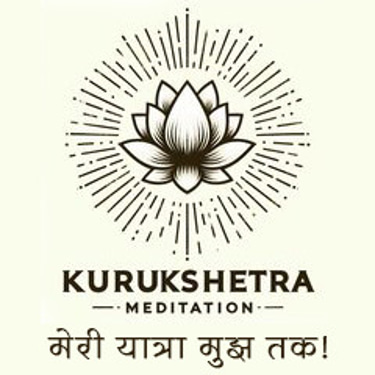माण्डूक्य उपनिषद
"Meditation Stages"
BLOG
12/10/20241 मिनट पढ़ें
माण्डूक्य उपनिषद
माण्डूक्य उपनिषद वेदांत का एक महत्वपूर्ण उपनिषद है, जो आथर्ववेद से लिया गया है। यह उपनिषद ब्रह्मज्ञान, आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माण्डूक्य उपनिषद में चार आध्यात्मिक अवस्थाएँ (States of Consciousness) और अहंकार (Self, Ego) के विभिन्न रूपों का विवरण है। यह उपनिषद आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गहन दार्शनिक विचार प्रस्तुत करता है।
माण्डूक्य उपनिषद का परिचय:
माण्डूक्य उपनिषद केवल 12 श्लोकों का है, लेकिन इसके विचार बहुत गहरे और सूक्ष्म हैं। इस उपनिषद में अहंकार (self), आत्मा (Atman), और ब्रह्म (Brahman) के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। यह उपनिषद विशेष रूप से आध्यात्मिक जागरूकता (spiritual awareness) और आत्म-समझ की दिशा में मार्गदर्शन देता है।
माण्डूक्य उपनिषद के प्रमुख विचार:
1. आध्यात्मिक अवस्थाएँ (States of Consciousness)
माण्डूक्य उपनिषद के अनुसार, मनुष्य की चार अवस्थाएँ होती हैं, जो उसकी चेतना के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये चार अवस्थाएँ हैं:
जाग्रत अवस्था (Waking State):
यह वह अवस्था है, जब व्यक्ति अपने शरीर और बाहरी संसार के प्रति जागरूक होता है। उसे अपनी इंद्रियों के माध्यम से भौतिक संसार की अनुभूति होती है। इस अवस्था में हम वस्तुओं को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं। यह "वाइश्वर" (Vaishvānara) रूप में प्रकट होता है।स्वप्न अवस्था (Dream State):
स्वप्न अवस्था में व्यक्ति अपनी इंद्रियों से स्वतंत्र होता है, लेकिन वह अपने भीतर के मन और इच्छाओं के आधार पर स्वप्न देखता है। यह अवस्था शुद्ध रूप से मानसिक होती है, जहां मन अपने विचारों, इच्छाओं और भूतकाल के अनुभवों को जोड़कर स्वप्न निर्मित करता है। इस अवस्था में व्यक्ति बाहर की दुनिया से अवगत नहीं होता। इसे "तैजस" (Taijasa) रूप कहा गया है।सुषुप्ति अवस्था (Deep Sleep State):
सुषुप्ति वह अवस्था है, जिसमें व्यक्ति न तो स्वप्न देखता है और न ही बाहर के संसार के बारे में जागरूक होता है। यह शांति और विश्राम की अवस्था होती है, जहां आत्मा पूर्णतया शांत और स्थिर रहती है। इस अवस्था में केवल चेतन्य के एकल रूप का अनुभव होता है। इसे "पारमात्मा" (Prājna) रूप कहा गया है।तुरीय अवस्था (The Fourth State):
यह अवस्था जाग्रत, स्वप्न, और सुषुप्ति से परे है, और इसे "आध्यात्मिक चेतना" का सर्वोत्तम रूप कहा जाता है। तुरीय अवस्था में व्यक्ति ब्रह्म के साथ एकाकार होता है। यह एक प्रकार की शांति, निर्विकल्प ध्यान और आत्मा का शुद्ध रूप है। यह ब्रह्म का अनुभव होता है, और इसमें व्यक्ति अपने वास्तविक रूप को पहचानता है। इसे "तुरीय" (Turiya) रूप कहा जाता है।
2. अहंकार (Self-Ego) और ब्रह्म का अद्वैत रूप
माण्डूक्य उपनिषद में यह स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्म और आत्मा का भेद केवल एक मानसिक भ्रम है। जो आत्मा (अहम्) अपने आप को शरीर और मन से पृथक समझती है, वह अहंकार (self-ego) के माध्यम से दुनिया को देखती है। जबकि ब्रह्म, जो निराकार और शाश्वत है, हर जगह व्याप्त है। आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं है; यह केवल हमारे अहंकार के कारण प्रतीत होता है। जब व्यक्ति अपनी वास्तविक आत्मा को पहचानता है, तो वह ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है।
3. अहं ब्रह्मास्मि (Aham Brahmasmi) – मैं ब्रह्म हूँ
माण्डूक्य उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत सिद्धांत का खुलासा किया गया है। उपनिषद के अंतिम श्लोक में यह विचार व्यक्त किया गया है कि "अहं ब्रह्मास्मि" यानी "मैं ब्रह्म हूँ"। यह आत्म-साक्षात्कार का सर्वोत्तम रूप है, जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और यह समझता है कि वह केवल एक भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि वह ब्रह्म का अंश है।
यह विचार उपनिषद में दर्शाता है कि हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वह केवल ब्रह्म के भिन्न-भिन्न रूप हैं। जब हम तुरीय अवस्था में पहुँचते हैं, तो हम ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं और हम वास्तविकता को बिना किसी भेदभाव के पहचानते हैं।
माण्डूक्य उपनिषद का उद्देश्य:
आध्यात्मिक जागरूकता: माण्डूक्य उपनिषद का मुख्य उद्देश्य आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत रूप को समझाना है। यह उपनिषद हमें यह सिखाता है कि बाहरी संसार और शरीर की अवस्थाएँ केवल भ्रम हैं, और हमारी असली पहचान ब्रह्म है।
चार अवस्थाओं का ज्ञान: यह उपनिषद चार अवस्थाओं (जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, और तुरीय) के माध्यम से चेतना की गहरी समझ प्रदान करता है। इन अवस्थाओं के अनुभव से हम अपनी आत्मा और ब्रह्म के असली स्वरूप को पहचान सकते हैं।
अहंकार की समाप्ति: माण्डूक्य उपनिषद यह भी सिखाता है कि अहंकार (ego) के माध्यम से हम स्वयं को ब्रह्म से पृथक मानते हैं। जब अहंकार समाप्त हो जाता है, तो आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं रह जाता, और व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है।
मुक्ति (मोक्ष): माण्डूक्य उपनिषद का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। यह उपनिषद यह स्पष्ट करता है कि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने से हम जन्म-मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं और आत्मा का शाश्वत स्वरूप पहचान सकते हैं।
माण्डूक्य उपनिषद वेदांत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषद है, जो आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत रूप को समझाने के लिए चार अवस्थाओं के माध्यम से गहरे दर्शन की ओर मार्गदर्शन करता है। इसमें चेतना के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है, जो आत्मा के शुद्ध रूप और ब्रह्म के साथ उसकी एकता को दिखाता है। आध्यात्मिक जागरूकता और अहंकार से मुक्ति के माध्यम से हम ब्रह्म के सत्य को जान सकते हैं और जीवन की वास्तविकता को पहचान सकते हैं।
माण्डूक्य उपनिषद के गहन विचार अत्यंत दार्शनिक और आत्मज्ञान से संबंधित हैं। यह उपनिषद आत्मा (Atman) और ब्रह्म (Brahman) के अद्वैत स्वरूप को प्रकट करता है, जो वेदांत दर्शन का एक केंद्रीय तत्व है। माण्डूक्य उपनिषद के विचारों को समझने के लिए हमें इसकी चार आध्यात्मिक अवस्थाओं (States of Consciousness) को गहरे से समझना होगा, जो आत्मा की शुद्ध और परम अवस्था को दर्शाती हैं।
इस उपनिषद में ब्रह्म के निराकार, शाश्वत और सर्वव्यापी रूप के बारे में भी बताया गया है। आइए, माण्डूक्य उपनिषद के गहन विचारों को विस्तार से समझें:
1. चार अवस्थाओं की अवधारणा (Four States of Consciousness)
माण्डूक्य उपनिषद में आध्यात्मिक अवस्थाएँ आत्मा की विभिन्न रूपों में चेष्टाएँ होती हैं। ये अवस्थाएँ केवल मानसिक या भौतिक नहीं हैं, बल्कि यह आत्मा और ब्रह्म के संबंध को स्पष्ट करने के उपाय हैं। ये चार अवस्थाएँ हैं:
1.1. जाग्रत अवस्था (Waking State)
जाग्रत अवस्था वह स्थिति है, जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों के माध्यम से भौतिक संसार के संपर्क में होता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने शरीर और संसार से पूरी तरह से जुड़ा हुआ महसूस करता है। जाग्रत अवस्था में मनुष्य का अहंकार प्रबल रहता है और वह बाहरी जगत के वस्तुओं के प्रति जागरूक होता है। इस अवस्था में ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप का अनुभव नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति इंद्रियदृष्टि से सब कुछ देखता है और अनुभव करता है।
1.2. स्वप्न अवस्था (Dream State)
स्वप्न अवस्था में व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों से मुक्त हो जाता है, लेकिन वह अपने भीतर के विचारों, इच्छाओं और कल्पनाओं के माध्यम से स्वप्न देखता है। यह अवस्था केवल मानसिक है, और बाहरी संसार से कोई संपर्क नहीं होता। स्वप्नों में व्यक्ति को उसके भीतर के अनुभव, अवचेतन और स्मृतियाँ प्रकट होती हैं। यह अवस्था असल में मानसिक भ्रम है, जहां ब्रह्म का वास्तविक रूप नहीं दिखाई देता। स्वप्न अवस्था में मनुष्य को अपने आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं दिखता।
1.3. सुषुप्ति अवस्था (Deep Sleep State)
सुषुप्ति वह अवस्था है, जब व्यक्ति न तो स्वप्न देखता है और न ही बाहरी संसार से कोई जागरूकता होती है। यह शांति की अवस्था है, जहां आत्मा शुद्धता के साथ गहरी निद्रा में होती है। यह वह स्थिति है, जब व्यक्ति केवल अपने अस्तित्व की शुद्धता को अनुभव करता है। सुषुप्ति अवस्था में व्यक्ति का अहंकार नष्ट हो जाता है और वह एक प्रकार से ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। यह अवस्था स्वाभाविक रूप से ब्रह्म के साक्षात्कार के निकट होती है, लेकिन यह एक स्थायी स्थिति नहीं है।
1.4. तुरीय अवस्था (The Fourth State)
तुरीय अवस्था चारों अवस्थाओं से परे है। यह शुद्ध, निराकार और अद्वितीय चेतना का रूप है, जिसे ब्रह्म या आध्यात्मिक चेतना के रूप में जाना जाता है। यह अवस्था कोई भी भौतिक या मानसिक द्वंद्व से मुक्त है, और इसमें व्यक्ति को आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का अनुभव होता है। तुरीय अवस्था में व्यक्ति को ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, और वह समझता है कि वह ब्रह्म का अंश है। यह अवस्था मोक्ष की ओर एक कदम होती है, जहां व्यक्ति आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करता है और बंधनों से मुक्त हो जाता है।
2. अहं ब्रह्मास्मि (Aham Brahmasmi) - मैं ब्रह्म हूँ
माण्डूक्य उपनिषद का सबसे गहन विचार "अहं ब्रह्मास्मि" है, जिसका अर्थ है, "मैं ब्रह्म हूँ"। यह विचार वेदांत दर्शन का मूल है, जो बताता है कि आत्मा और ब्रह्म का कोई भेद नहीं है। उपनिषद यह स्पष्ट करता है कि ब्रह्म निराकार, शाश्वत और सर्वव्यापी है, और मनुष्य का आत्मा भी उसी ब्रह्म का अंश है। जब व्यक्ति अपने अहंकार (ego) से पार होकर अपनी वास्तविकता को पहचानता है, तब वह आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत रूप का अनुभव करता है।
यह विचार आत्मज्ञान की उच्चतम अवस्था का प्रतीक है, जहां व्यक्ति समझता है कि वह केवल एक भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि वह ब्रह्म का ही अंश है। "अहं ब्रह्मास्मि" का अर्थ यह है कि ब्रह्म का सत्य केवल आत्मा में छुपा हुआ है और आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है।
3. ब्रह्म और आत्मा का अद्वैत सिद्धांत (The Non-Duality of Atman and Brahman)
माण्डूक्य उपनिषद का एक और गहन विचार यह है कि आत्मा (Atman) और ब्रह्म (Brahman) एक ही हैं, और कोई भेद नहीं है। उपनिषद में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है कि जो कुछ भी हम देखते हैं, वह सब ब्रह्म का ही रूप है। हमारे शरीर, हमारे विचार, हमारी इंद्रियाँ — सब ब्रह्म के विविध रूप हैं। हमारे अहंकार के कारण हमें यह भेद दिखाई देता है, लेकिन असल में आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। जब अहंकार समाप्त हो जाता है, तो ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और आत्मा ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती है।
यह अद्वैत सिद्धांत माण्डूक्य उपनिषद का केंद्रीय संदेश है, और यह दर्शाता है कि वास्तविकता केवल एक है, और वह है ब्रह्म।
4. मुक्ति (Moksha) और आत्मा का वास्तविक स्वरूप
माण्डूक्य उपनिषद में मुक्तिके बारे में भी गहन विचार किए गए हैं। यह उपनिषद स्पष्ट करता है कि मुक्ति (मोक्ष) तब प्राप्त होती है, जब व्यक्ति अपने आत्मा का शुद्ध रूप पहचानता है और अहंकार से मुक्त हो जाता है। मुक्त व्यक्ति ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है और जन्म-मृत्यु के चक्र से बाहर निकल आता है।
यह उपनिषद यह भी बताता है कि मुक्ति केवल ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त होती है। जब व्यक्ति सच्चे ज्ञान का अभ्यास करता है और आत्मा के वास्तविक रूप को पहचानता है, तब वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है।
माण्डूक्य उपनिषद के गहन विचारों में मुख्य रूप से आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत रूप को स्थापित किया गया है। इसमें चार अवस्थाओं के माध्यम से चेतना के विभिन्न रूपों का विवरण किया गया है, जिनका लक्ष्य आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना और ब्रह्म के साथ एकात्मता को महसूस करना है। यह उपनिषद आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करता है, जहां आत्मा और ब्रह्म का भेद मिट जाता है, और व्यक्ति ब्रह्म का साक्षात्कार करता है।
माण्डूक्य उपनिषद में कोई विशेष "कहानी" नहीं है, जैसे कि अन्य उपनिषदों में शिष्य और गुरु के संवाद होते हैं। इसके बजाय, यह एक बहुत संक्षिप्त और गहन दार्शनिक पाठ है जो ब्रह्मज्ञान, आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप को समझाने के लिए उपयोग किए गए विचारों और सिद्धांतों का प्रस्तुतीकरण है। यह उपनिषद मुख्य रूप से आत्मा के चार अवस्थाओं, उनके अर्थ और तुरीय अवस्था (चौथी अवस्था) के महत्व को स्पष्ट करता है।
हालाँकि, माण्डूक्य उपनिषद की रचनात्मक संरचना में एक काव्यात्मक रूप में आत्मज्ञान की गहरी स्थिति की प्रस्तुति की गई है, जिसे एक गुरु शिष्य को उपदेश देने के रूप में समझा जा सकता है। इस उपनिषद का उद्देश्य आत्मा (अहम्) और ब्रह्म (ब्रह्म) के अद्वैत सिद्धांत को प्रस्तुत करना है, जो "अहं ब्रह्मास्मि" (मैं ब्रह्म हूँ) के सिद्धांत पर आधारित है।
यहाँ एक रूपक के रूप में इसे एक गुरु और शिष्य के संवाद में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें गुरु शिष्य को आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप के बारे में सिखाते हैं। चलिए, इसे इस तरह समझते हैं:
माण्डूक्य उपनिषद का कथात्मक रूप
गुरु और शिष्य का संवाद
गुरु एक शिष्य को आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए उपदेश देते हैं। शिष्य गुरु से आत्मा और ब्रह्म के बारे में प्रश्न करता है। गुरु शिष्य को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आत्मा (अहम्) और ब्रह्म (ब्रह्म) एक ही हैं, और जो भेद हमें दिखाई देता है, वह केवल मानसिक भ्रांति है। गुरु ने शिष्य से पूछा, "तुम कौन हो?" शिष्य उत्तर देता है, "मैं आत्मा हूँ," तब गुरु उसे समझाते हैं कि जो तुम समझ रहे हो, वह केवल भौतिक शरीर और मन का रूप है, और वास्तविकता कहीं अधिक गहरी है।चार अवस्थाएँ (States of Consciousness)
गुरु शिष्य को यह बताते हैं कि आत्मा की चार अवस्थाएँ होती हैं:जाग्रत अवस्था (Waking state): यह वह अवस्था है, जब मनुष्य बाहरी दुनिया के संपर्क में होता है और इंद्रियाँ उसे भौतिक वस्तुओं का अनुभव कराती हैं। इस अवस्था में हम शरीर और मन के द्वारा संसार का अनुभव करते हैं।
स्वप्न अवस्था (Dream state): स्वप्नों में व्यक्ति मानसिक और आंतरिक अनुभवों से जुड़ा होता है, परंतु वह बाहरी संसार से अलग रहता है। यह अवस्था आत्मा की सूक्ष्मता को दर्शाती है।
सुषुप्ति अवस्था (Deep sleep state): सुषुप्ति अवस्था में व्यक्ति बाहरी संसार से पूरी तरह से अज्ञात रहता है और केवल आत्मा की शुद्ध अवस्था का अनुभव करता है। इसमें वह न तो सपने देखता है और न ही जागता है।
तुरीय अवस्था (The fourth state): यह सबसे उच्च अवस्था है, जब व्यक्ति ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। यह अवस्था आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप को अनुभव करने की है। इसमें व्यक्ति ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और समझता है कि आत्मा और ब्रह्म का भेद केवल एक भ्रांति है।
अहं ब्रह्मास्मि (Aham Brahmasmi)
गुरु शिष्य को यह सिखाते हैं कि आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं है। जब शिष्य इन अवस्थाओं के माध्यम से आत्मा का सत्य जानता है, तब वह यह समझता है कि वह स्वयं ब्रह्म है। यह सत्यज्ञान शिष्य को "अहं ब्रह्मास्मि" (मैं ब्रह्म हूँ) के रूप में मिलता है, और शिष्य अब किसी भौतिक रूप से नहीं, बल्कि शाश्वत और शुद्ध रूप से आत्मा को पहचानता है।आध्यात्मिक मुक्ति
जब शिष्य आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप का साक्षात्कार करता है, तो वह मुक्ति (मोक्ष) प्राप्त कर लेता है। अब वह जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और शाश्वत सत्य को जानता है। गुरु के उपदेशों से शिष्य ने यह सीखा कि मुक्ति केवल ब्रह्मज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है।
माण्डूक्य उपनिषद की कहानी एक गुरु-शिष्य संवाद के रूप में है, जहाँ गुरु शिष्य को आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत रूप को समझाते हैं। यह उपनिषद मुख्य रूप से आत्मा की चार अवस्थाओं (जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, और तुरीय) के माध्यम से आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान के रास्ते को स्पष्ट करता है। माण्डूक्य उपनिषद यह सिखाता है कि हमारे अहंकार और भौतिक दुनिया का भ्रम समाप्त होते ही हम ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं और सत्य को पहचानते हैं।
हमारा उद्देश्य केवल सजगता बढ़ाना है ,हम जन साधारण को संतो, ध्यान विधियों ,ध्यान साधना से संबन्धित पुस्तकों के बारे मे जानकारी , इंटरनेट पर मौजूद सामग्री से जुटाते है । हम किसी धर्म ,संप्रदाय ,जाति , कुल ,या व्यक्ति विशेष की मान मर्यादा को ठेस नही पहुंचाते है । फिर भी जाने अनजाने , यदि किसी को कुछ सामग्री सही प्रतीत नही होती है , कृपया हमें सूचित करें । हम उस जानकारी को हटा देंगे ।
website पर संतो ,ध्यान विधियों , पुस्तकों के बारे मे केवल जानकारी दी गई है , यदि साधकों /पाठकों को ज्यादा जानना है ,तब संबन्धित संस्था ,संस्थान या किताब के लेखक से सम्पर्क करे ।
© 2024. All rights reserved.