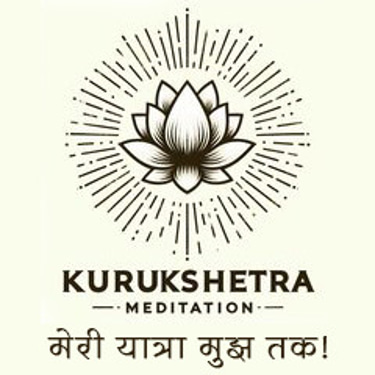गुरु गोरखनाथ
नाथ संप्रदाय
SAINTS
10/17/20241 मिनट पढ़ें
नाथ संप्रदाय: नाथ संप्रदाय का आरंभ 8वीं-9वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। इसकी नींव गुरु मत्स्येन्द्रनाथ ने रखी , जिन्हें भगवान शिव से तंत्र साधनाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ था। मत्स्येन्द्रनाथ के शिष्य गुरु गोरखनाथ ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और इसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचारित किया। गोरखनाथ ने योग, तंत्र और ध्यान की गहन साधनाओं को साधारण लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने हठयोग की विधियों को सरल और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया।
यह भारतीय योग और साधना की एक प्रमुख धारा है, जिसका आधार शिव उपासना, तांत्रिक साधनाएँ और योगिक क्रियाएँ हैं। यह संप्रदाय मुख्यतः गुरु मत्स्येन्द्रनाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ द्वारा स्थापित और विकसित किया गया। नाथ संप्रदाय का गहन संबंध शिव से है, जिन्हें इस परंपरा में "आदिगुरु" के रूप में पूजा जाता है। नाथ योगियों का प्रमुख उद्देश्य योग, ध्यान और तंत्र की साधनाओं के माध्यम से आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करना है।
नाथ संप्रदाय में प्रमुख संतों की एक गुरु-शिष्य परंपरा रही है, जिसमें गुरु अपने शिष्यों को योग, साधना और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं।
नाथ संप्रदाय के प्रमुख सिद्धांत
नाथ संप्रदाय की शिक्षाएँ योग, तंत्र, और आत्मज्ञान के मार्ग पर आधारित हैं। इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं:
1. हठयोग: नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा योगदान हठयोग की विधियों का विकास और प्रचार है। हठयोग का मुख्य उद्देश्य शरीर और मन को साधना के माध्यम से शुद्ध करना है ताकि साधक आत्मज्ञान प्राप्त कर सके। नाथ योगियों के अनुसार, शरीर और मन को नियंत्रित किए बिना आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता।
2. कुंडलिनी जागरण: नाथ संप्रदाय में कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना एक महत्वपूर्ण साधना मानी जाती है। कुंडलिनी शक्ति शरीर के मूलाधार चक्र में स्थित एक सुप्त शक्ति है, जिसे योग के माध्यम से जागृत कर साधक अपने शरीर के विभिन्न चक्रों को पार कर सकता है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है।
3. शिव-शक्ति सिद्धांत: नाथ संप्रदाय शिव और शक्ति के एकात्मक सिद्धांत पर आधारित है। इसमें शिव को सर्वोच्च देवता माना जाता है, और शक्ति को उनकी शक्ति के रूप में पूजा जाता है। साधक का उद्देश्य शिव और शक्ति (पुरुष और प्रकृति) के मिलन के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना होता है।
4. गुरु-शिष्य परंपरा: नाथ संप्रदाय में गुरु का अत्यधिक महत्व है। गुरु को साधक के आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है, जो शिष्य को आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। नाथ योगियों की शिक्षा में गुरु की आज्ञा और शिक्षाओं का पालन अत्यावश्यक माना जाता है।
5. तांत्रिक साधनाएँ: नाथ संप्रदाय में तंत्र साधनाओं का प्रमुख स्थान है। तंत्र साधनाएँ शरीर और मन की शक्ति को जागृत करने के लिए होती हैं। नाथ योगियों के अनुसार, तंत्र साधना के माध्यम से साधक संसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है।
6. अद्वैतवाद: नाथ संप्रदाय अद्वैतवाद पर आधारित है, जिसमें आत्मा और परमात्मा को एक ही माना जाता है। नाथ योगियों के अनुसार, संसार और आत्मा के बीच कोई भिन्नता नहीं है, और यह समझने पर ही साधक मोक्ष प्राप्त कर सकता है।
नाथ योगियों की विशेषताएँ
नाथ योगियों को "कानफटा" योगी कहा जाता है, क्योंकि दीक्षा के समय उनके कान छिदवाए जाते हैं। यह परंपरा नाथ संप्रदाय में दीक्षा का प्रतीक मानी जाती है। कान छिदवाने की यह प्रथा योगियों के संसारिक जीवन से विरक्त होने और साधना के मार्ग पर चलने का प्रतीक होती है। नाथ योगी अक्सर तपस्वी जीवन व्यतीत करते हैं, शरीर और मन पर कठोर अनुशासन रखते हैं, और योग, प्राणायाम, और ध्यान का गहन अभ्यास करते हैं।
नाथ योगियों का पहनावा भी विशिष्ट होता है। वे अपने शरीर को भभूत (राख) से ढकते हैं, जो शिव की साधना का प्रतीक है। उनके पास एक लाठी, काठ का माला और साधु वेश होता है। वे साधारण और तपस्वी जीवन जीते हैं, भिक्षा पर जीवन यापन करते हैं, और समाज से अलग रहते हुए ध्यान और योग साधना करते हैं।
नाथ संप्रदाय के प्रमुख गुरु
नाथ संप्रदाय की गुरु-शिष्य परंपरा में कई महान संत और योगी हुए हैं, जिन्होंने इस परंपरा को समृद्ध बनाया। इनमें प्रमुख गुरु इस प्रकार हैं:
1. गुरु मत्स्येन्द्रनाथ: नाथ संप्रदाय के संस्थापक, जिन्होंने तंत्र साधना का प्रसार किया।
2. गुरु गोरखनाथ: मत्स्येन्द्रनाथ के शिष्य, जिन्होंने हठयोग और नाथ संप्रदाय को संगठित किया और इसे जनसाधारण के बीच लोकप्रिय बनाया।
3. चौरंगीनाथ: गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक, जिन्होंने साधना के माध्यम से महान उपलब्धियाँ प्राप्त कीं।
4. झूलेलाल नाथ: वे नाथ योगियों के प्रमुख संत माने जाते हैं, जो सिंधु घाटी में पूजित हैं।
नाथ संप्रदाय के ग्रंथ
नाथ संप्रदाय के अनुयायी विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जिनमें योग, तंत्र, और ध्यान की विधियाँ वर्णित हैं। कुछ प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं:
1. गोरक्ष संहिता: गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित, जिसमें हठयोग की विधियों और सिद्धांतों का वर्णन किया गया है।
2. हठयोग प्रदीपिका: स्वामी स्वात्माराम द्वारा रचित, यह हठयोग के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, जिसमें योग के विभिन्न आसनों, प्राणायाम और ध्यान का वर्णन किया गया है।
3. सिद्ध सिद्धांत पद्धति: यह एक महत्वपूर्ण नाथ संप्रदाय ग्रंथ है, जिसमें साधना, ध्यान और आत्मज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया गया है।
4. शिव संहिता: इस ग्रंथ में तांत्रिक साधनाओं और योग के माध्यम से कुंडलिनी जागरण का विस्तृत वर्णन मिलता है।
गुरु गोरखनाथ
भारतीय संत और योग परंपरा के महान आध्यात्मिक गुरु रहे है । वे नाथ संप्रदाय के प्रमुख संत माने जाते हैं और हठयोग के प्रसार में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। गोरखनाथ का जीवन, उनके उपदेश, और उनकी विचारधारा ने भारतीय धार्मिक और योग परंपराओं पर गहरा प्रभाव डाला है। उनके अनुयायी उन्हें एक दिव्य अवतार और सिद्ध योगी मानते हैं जिन्होंने मोक्ष (आत्मज्ञान) प्राप्त किया था।
प्रारंभिक जीवन और किंवदंतियाँ
गुरु गोरखनाथ के जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में कई किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, और उनके जन्म का सही समय स्पष्ट नहीं है। यह माना जाता है कि वे 11वीं या 12वीं शताब्दी में अवतरित हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि गोरखनाथ, नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे और उन्हें मत्स्येंद्रनाथ द्वारा योग मार्ग में दीक्षा दी गई थी।
गुरु गोरखनाथ को कई लोग एक चमत्कारिक अवतार मानते हैं, और कुछ कथाओं के अनुसार वे किसी सामान्य जन्म से नहीं बल्कि योग शक्ति से प्रकट हुए थे। इस कारण से उन्हें एक दिव्य और अलौकिक योगी माना जाता है।
नाथ संप्रदाय: नाथ संप्रदाय शैव परंपरा पर आधारित है, जिसमें शिव की उपासना, योग साधना और तंत्र का समावेश होता है। गोरखनाथ ने नाथ योगियों के आदर्शों को स्थापित और प्रचारित किया। यह संप्रदाय शारीरिक अनुशासन, मानसिक स्थिरता, और आत्मज्ञान पर आधारित है।
नाथ संप्रदाय का उद्देश्य मानव जीवन में आध्यात्मिकता लाना और योग के माध्यम से शरीर और मन को शुद्ध करना है। गुरु गोरखनाथ ने विशेष रूप से हठयोग का प्रचार किया, जो शरीर और मन के नियंत्रण पर आधारित एक योग प्रणाली है।
गुरु गोरखनाथ के जीवन से जुड़ी कई कहानियाँ हैं जो उनके चमत्कारिक और गहरे आध्यात्मिक ज्ञान, तपस्या, योग साधना, और उनके शिष्यों के प्रति उनके अद्भुत प्रेम को दर्शाती हैं। गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं और उन्हें महायोगी शिव का अवतार भी माना गया है।
गुरु गोरखनाथ जीवन से जुड़ी कुछ प्रमुख कहानियाँ :
1. मछंदरनाथ के शिष्य बनने की कहानी
- कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ का जन्म एक विशेष साधना के परिणामस्वरूप हुआ। उनकी माँ ने महायोगी मछंदरनाथ से आशीर्वाद प्राप्त किया था कि उनके गर्भ में एक महान योगी का जन्म होगा। गुरु गोरखनाथ ने महायोगी मछंदरनाथ को अपना गुरु मानकर उनसे योग और तंत्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया।
- जब गोरखनाथ ने मछंदरनाथ को अपना गुरु मान लिया, तो उन्होंने जीवनभर अपने गुरु के प्रति आदर और समर्पण का भाव रखा। वे अपने गुरु के हर आदेश का पालन करते और अपने जीवन में सादगी और तपस्या का मार्ग अपनाते।
2. भिक्षा में कुछ न लेने का संकल्प
- गोरखनाथ ने अपने तपस्वी जीवन में भिक्षा माँगते समय एक संकल्प लिया कि वे भिक्षा में अन्न का दाना तक नहीं लेंगे, केवल "गोरख" शब्द लेंगे। इस प्रकार वे अपने अनुयायियों को यह सिखाना चाहते थे कि तपस्वी जीवन में सांसारिक वस्तुओं का त्याग आवश्यक है।
- एक बार एक महिला ने उन्हें भिक्षा में भोजन देना चाहा, लेकिन गोरखनाथ ने कहा, "मुझे केवल 'गोरख' चाहिए।" इस बात से प्रेरित होकर, महिला ने उन्हें गोरख शब्द के साथ आशीर्वाद दिया। गोरखनाथ ने यह संदेश दिया कि तपस्वी जीवन में त्याग और संतोष का पालन करना चाहिए।
3. कपिला गाय का चमत्कार
- एक बार गुरु गोरखनाथ ने एक गाँव में जाकर अपनी योग शक्ति से एक मृत गाय को पुनर्जीवित किया। यह गाय "कपिला गाय" के नाम से प्रसिद्ध है। इस चमत्कार से प्रभावित होकर गाँव के लोग उनके अनुयायी बन गए और गोरखनाथ के प्रति श्रद्धा से भर गए।
- यह घटना उनके महान योग और साधना की शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि योग साधना के माध्यम से व्यक्ति अद्भुत शक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसे परोपकार के लिए उपयोग करना चाहिए।
4. राजा भर्तृहरि को सन्यास दिलाना
- गोरखनाथ के एक प्रसिद्ध शिष्य राजा भर्तृहरि थे। भर्तृहरि अपने राजा जीवन से संतुष्ट नहीं थे और संसार से विरक्त होकर सन्यास लेने का निर्णय कर चुके थे। गोरखनाथ ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें सन्यास और योग का मार्ग दिखाया।
- गोरखनाथ ने भर्तृहरि को सिखाया कि सांसारिक जीवन में मोह-माया और विषय-वासनाएँ आत्मा की मुक्ति में बाधा उत्पन्न करती हैं। भर्तृहरि ने उनके मार्गदर्शन में योग साधना की और एक महान योगी बने।
5. ब्रह्मराक्षस का उद्धार
- एक बार गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे, जहाँ एक ब्रह्मराक्षस का वास था। यह राक्षस एक साधु था जो साधना में गलती करने के कारण श्रापित हो गया था। गोरखनाथ ने अपनी तपस्या और योग शक्ति से उसे मुक्ति दिलाई और उसे अपने मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी।
- इस घटना ने यह दिखाया कि गोरखनाथ अपने ज्ञान और करुणा का उपयोग दूसरों की सहायता करने में करते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी सिखाया कि योग की शक्ति का उपयोग सेवा और उद्धार के लिए करना चाहिए।
हठ योग का आरम्भ
- गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया और इसे शारीरिक और मानसिक शुद्धि का साधन बताया। उन्होंने अपने शिष्यों को हठ योग की विभिन्न मुद्राओं, आसनों, और प्राणायाम की शिक्षा दी, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में सहायक हैं।
- उनके द्वारा प्रवर्तित हठ योग में शरीर को कठोरता, मानसिक स्थिरता, और ईश्वर से एकत्व प्राप्त करने का मार्ग बताया गया। गोरखनाथ के इस योग पद्धति को नाथ संप्रदाय में व्यापक रूप से अपनाया गया।
7. अलख निरंजन का प्रचार
- गुरु गोरखनाथ ने "अलख निरंजन" का संदेश दिया, जिसका अर्थ है कि ईश्वर निर्गुण और निराकार है। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि ईश्वर को किसी विशेष रूप में नहीं बाँधा जा सकता और उसे केवल आत्मज्ञान और साधना के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है।
- "अलख निरंजन" का जाप गोरखनाथ के अनुयायियों में लोकप्रिय हो गया, और यह संदेश गोरखनाथ के निर्गुण ईश्वर की आराधना और मोक्ष प्राप्ति के सिद्धांत को दर्शाता है।
8. बिना जल के घड़ा भरने की कहानी
- एक बार गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य एक गाँव में पहुँचे, जहाँ एक औरत उनसे मिलने आई और उन्हें जल से भरा हुआ घड़ा भिक्षा में देने का प्रस्ताव दिया। गोरखनाथ ने उसे मना करते हुए कहा कि वह उन्हें एक खाली घड़ा दे, और वे उसे अपनी योग शक्ति से जल से भर देंगे।
- गाँव वालों ने इस चमत्कार को देखा और गोरखनाथ के प्रति और भी अधिक श्रद्धा से भर गए। इस घटना से यह प्रतीत होता है कि गोरखनाथ में अद्भुत योगिक शक्ति थी, परंतु वे इसे दिखावा करने के लिए नहीं बल्कि लोगों को सत्य के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करते थे।
9. साधना की कठिन परीक्षाएँ
- गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों को साधना में विभिन्न परीक्षाएँ लेकर उन्हें दृढ़ और सच्चा योगी बनाने का प्रयास करते थे। वे अपने शिष्यों को कठोर अभ्यास और साधना से गुजरने के लिए प्रेरित करते ताकि वे आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें।
- एक कथा के अनुसार, उन्होंने अपने शिष्यों को एक बार अग्नि में तपने का आदेश दिया ताकि वे भय, दुःख और मोह से मुक्त हो सकें। इस प्रकार की कठिन परीक्षाओं के माध्यम से वे अपने शिष्यों को उच्चतम आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करते थे।
गुरु गोरखनाथ के जीवन की ये कहानियाँ उनकी योगिक शक्ति, साधना, सेवा, और अध्यात्म की गहराई को दर्शाती हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को निस्वार्थ सेवा, संयम, और आत्म-साक्षात्कार के महत्व को सिखाया। उनके उपदेश और जीवन की घटनाएँ भारतीय साधना परंपरा में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं और उनके द्वारा प्रवर्तित नाथ संप्रदाय का अनुसरण आज भी किया जाता है।
गुरु गोरखनाथ की शिक्षाएँ और दर्शन
गुरु गोरखनाथ का ध्यान योग, साधना, और आत्म-नियंत्रण पर था। उनके कुछ प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं:
1. योग और अनुशासन: गोरखनाथ ने योग को आत्मज्ञान प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने हठयोग के अंतर्गत कई आसनों, प्राणायाम (सांस नियंत्रण) और ध्यान की विधियों को प्रकट किया। उनका मानना था कि योग के माध्यम से साधक शरीर और मन को नियंत्रित कर सकता है।
2. वैराग्य (विरक्ति): गोरखनाथ ने संसारिक इच्छाओं और भौतिक सुखों से विरक्ति की शिक्षा दी। उनका मानना था कि भौतिक सुखों से मोहित व्यक्ति आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता।
3. शिव और शक्ति का मिलन: उनके दर्शन में शिव (चेतना) और शक्ति (ऊर्जा) का मिलन मुख्य भूमिका निभाता है। उनका मानना था कि मानव शरीर एक मंदिर है और इसके अंदर ही ईश्वर का निवास है। योगी का उद्देश्य इस दिव्य शक्ति को जागृत करना होता है।
4. अद्वैतवाद (अद्वितीयता): गोरखनाथ का दर्शन अद्वैतवाद पर आधारित था, जिसमें आत्मा (जीवात्मा) और परमात्मा में कोई भेद नहीं माना जाता। उनके अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही हैं और इस एकता का अनुभव ही मोक्ष है।
5. सामाजिक समानता और भाईचारा: गोरखनाथ ने जाति, धर्म, और वर्ग के भेदभाव को अस्वीकार किया। उनके शिष्यों में सभी वर्गों और जातियों के लोग शामिल थे, और उन्होंने मानवता की समानता पर जोर दिया।
हठयोग और गोरखनाथ
गोरखनाथ को हठयोग की विधियों का प्रवर्तक माना जाता है। उनके द्वारा या उनके शिष्यों द्वारा लिखित गोरक्ष संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति जैसी ग्रंथों में हठयोग के बारे में विस्तार से बताया गया है।
- गोरक्ष संहिता: इस ग्रंथ में हठयोग की विधियों, जैसे प्राणायाम (श्वास नियंत्रण), आसन (शारीरिक मुद्राएँ), और कुंडलिनी जागरण की चर्चा की गई है।
- सिद्ध सिद्धांत पद्धति: यह एक दार्शनिक ग्रंथ है, जिसमें आत्मा, ब्रह्मांड, और मोक्ष के विषय में चर्चा की गई है।
भारतीय धर्मों पर प्रभाव
गुरु गोरखनाथ के विचारों और शिक्षाओं का प्रभाव कई भारतीय धर्मों और परंपराओं पर देखा जा सकता है:
1. हिंदू धर्म: गोरखनाथ को हिंदू धर्म में एक महान संत और योगी के रूप में माना जाता है। उन्हें विशेष रूप से शैव परंपरा में उच्च स्थान प्राप्त है।
2. सिख धर्म: सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने नाथ योगियों के साथ संवाद किया था। "सिद्ध गोष्ठी" में गुरु नानक और नाथ योगियों के बीच की चर्चा का वर्णन है। हालांकि, गुरु नानक ने नाथ योगियों के कठोर तप को अस्वीकार किया, लेकिन उनके विचारों का आदर किया।
3. बौद्ध धर्म: गोरखनाथ का तांत्रिक बौद्ध धर्म (वज्रयान) पर भी प्रभाव पड़ा, खासकर नेपाल और तिब्बत में।
4. लोक परंपराएँ: गोरखनाथ का प्रभाव भारतीय लोक संस्कृति में भी देखा जा सकता है। उनके अनुयायी कानफटा योगी कहलाते हैं, जो उनके आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हैं।
गोरखनाथ मंदिर और विरासत
भारत और नेपाल में गोरखनाथ के कई मंदिर हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर है। यह नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है और यहाँ पर नाथ योगियों के अनेक धार्मिक आयोजन होते हैं।
गुरु गोरखनाथ के योग और साधना की परंपरा आज भी जीवित है। हठयोग का अभ्यास करने वाले योगी उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी शिक्षा ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में योग और आध्यात्मिक साधना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
नाथ संप्रदाय - नाथ संप्रदाय भारतीय योग और साधना की एक महत्वपूर्ण परंपरा है, जो मुख्य रूप से शिव उपासना, तांत्रिक साधनाओं, और योग की विभिन्न विधियों पर आधारित है। इस संप्रदाय के अनुयायी नाथ योगी कहलाते हैं। नाथ संप्रदाय का संस्थापक मत्स्येन्द्रनाथ को माना जाता है, जबकि इसके सबसे प्रमुख गुरु गुरु गोरखनाथ हैं, जिन्होंने इस परंपरा को व्यापक रूप से प्रसारित किया और इसे एक सुसंगठित रूप दिया।
नाथ संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ
नाथ संप्रदाय के अनुयायी कई ग्रंथों का अध्ययन और अनुसरण करते हैं, जिनमें योग, तंत्र और साधना के सिद्धांतों का वर्णन है। कुछ प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं:
1. गोरक्ष संहिता: यह ग्रंथ गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित मानी जाती है, जिसमें हठयोग की विधियों का विस्तृत वर्णन है।
2. सिद्ध सिद्धांत पद्धति: यह एक दार्शनिक ग्रंथ है, जिसमें आत्मा, परमात्मा, और मोक्ष के विषय पर चर्चा की गई है।
3. हठयोग प्रदीपिका: इस ग्रंथ में हठयोग की विधियों और सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जो नाथ संप्रदाय के योगियों द्वारा व्यापक रूप से अनुकरण किया जाता है।
हठयोग
हठयोग भारतीय योग परंपरा की एक प्रमुख शाखा है, जो शारीरिक और मानसिक अनुशासन के माध्यम से आत्म-साक्षात्कार और आध्यात्मिक उन्नति पर केंद्रित है। "हठ" शब्द का अर्थ होता है "बलपूर्वक" या "सख्ती से," जो संकेत करता है कि हठयोग साधक को शरीर और मन पर पूरा नियंत्रण प्राप्त करने के लिए कठोर साधना और अनुशासन अपनाना पड़ता है। इस योग प्रणाली का मुख्य उद्देश्य शरीर के माध्यम से मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करना है।
हठयोग का इतिहास और उत्पत्ति
हठयोग की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी और इसे गुरु गोरखनाथ और उनके गुरु मत्स्येन्द्रनाथ जैसे नाथ योगियों ने विकसित और प्रचारित किया। हठयोग को नाथ संप्रदाय के साधकों ने अत्यधिक महत्व दिया और इसे आत्म-साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति के साधन के रूप में देखा। गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित गोरक्ष संहिता और अन्य योग ग्रंथों में हठयोग की विधियों और सिद्धांतों का वर्णन मिलता है।
हठयोग के प्रमुख अंग
हठयोग मुख्य रूप से शारीरिक और मानसिक अनुशासन के माध्यम से साधक को आत्मसाक्षात्कार की ओर ले जाने पर आधारित है। इसके कुछ प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं:
1. आसन (शारीरिक मुद्राएँ): हठयोग में विभिन्न आसनों का अभ्यास किया जाता है, जो शरीर को स्थिर, लचीला, और सशक्त बनाते हैं। आसनों का उद्देश्य न केवल शरीर को स्वस्थ रखना है, बल्कि मन को स्थिर और ध्यानमग्न करने में भी सहायक होता है। प्रसिद्ध आसनों में पद्मासन, शवासन, सर्वांगासन आदि शामिल हैं।
2. प्राणायाम (श्वास नियंत्रण): प्राणायाम हठयोग का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें श्वास को नियंत्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य प्राण (जीवन ऊर्जा) को जागृत करना और उसे शरीर के विभिन्न अंगों में सही ढंग से प्रवाहित करना है। प्रमुख प्राणायाम तकनीकों में अनुलोम-विलोम, भस्त्रिका, और कपालभाति शामिल हैं।
3. शुद्धिकरण क्रियाएँ (षट्कर्म): हठयोग में शरीर को शुद्ध करने के लिए षट्कर्म (छह शुद्धिकरण क्रियाएँ) का अभ्यास किया जाता है। ये क्रियाएँ शरीर से विषाक्त तत्वों को निकालने और शरीर के विभिन्न अंगों को शुद्ध करने में मदद करती हैं। इसमें प्रमुख क्रियाएँ हैं:
- नेति (नाक की शुद्धि)
- धौति (पेट की शुद्धि)
- बस्ति (आंतों की शुद्धि)
- कपालभाति (मस्तिष्क की शुद्धि)
- नौली (पेट के अंगों की शुद्धि)
- त्राटक (दृष्टि की शुद्धि)
4. बंध (ऊर्जा नियंत्रण): बंध हठयोग की एक विशेष क्रिया है, जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों को एक विशेष स्थिति में रोका जाता है। इसका उद्देश्य शरीर के अंदर की ऊर्जा को नियंत्रित और संचालित करना है। प्रमुख बंधों में मूलबंध (मूलाधार क्षेत्र की जकड़न), उड्डियान बंध (नाभि क्षेत्र की जकड़न), और जालंधर बंध (गले की जकड़न) शामिल हैं।
5. मुद्राएँ: मुद्राओं का प्रयोग शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित और दिशा देने के लिए किया जाता है। यह उन्नत साधकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती हैं, जो कुंडलिनी जागरण या अन्य उच्चतर योगिक उद्देश्यों के लिए साधना करते हैं। प्रमुख मुद्राओं में महामुद्रा, महाबंध और योग मुद्रा शामिल हैं।
6. ध्यान: हठयोग का अंतिम और सर्वोच्च अंग ध्यान है। आसन, प्राणायाम, और अन्य क्रियाओं के अभ्यास के बाद साधक ध्यान की अवस्था में प्रवेश करता है, जिसमें मन शांत हो जाता है और साधक आत्मसाक्षात्कार की ओर बढ़ता है।
हठयोग का उद्देश्य
हठयोग का प्रमुख उद्देश्य आत्म-साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्त करना है। हठयोग में साधक शरीर को स्वस्थ, सशक्त और स्थिर बनाकर मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। यह योग शरीर को साधना का एक साधन मानता है, जिसमें शरीर और मन के सामंजस्य से आत्मज्ञान प्राप्त किया जाता है। हठयोग में यह माना जाता है कि जब तक शरीर और मन स्थिर और शुद्ध नहीं होते, तब तक आत्मिक उन्नति संभव नहीं होती।
हठयोग का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य शरीर में स्थित कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है। कुंडलिनी शक्ति को आधार चक्र (मूलाधार) में सोई हुई दिव्य शक्ति माना जाता है, जिसे योग के माध्यम से जागृत करके साधक चक्रों (शरीर के ऊर्जा केंद्रों) को पार कर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है।
हठयोग के प्रमुख ग्रंथ
हठयोग के सिद्धांतों और विधियों का वर्णन विभिन्न योग ग्रंथों में किया गया है। कुछ प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं:
1. हठयोग प्रदीपिका: यह स्वामी स्वात्माराम द्वारा 15वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें हठयोग के विभिन्न आसनों, प्राणायाम, मुद्राओं, और ध्यान की विधियों का विस्तृत वर्णन किया गया है।
2. गोरक्ष संहिता: गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित इस ग्रंथ में हठयोग की विधियों और सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। यह नाथ योगियों के लिए एक प्रमुख ग्रंथ है।
3. शिव संहिता: यह एक प्राचीन योग ग्रंथ है, जिसमें हठयोग के साथ-साथ राजयोग और तांत्रिक साधनाओं का भी उल्लेख है।
4. घेरंड संहिता: इस ग्रंथ में योग साधनाओं का व्यापक वर्णन किया गया है और इसे हठयोग के सिद्धांतों को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
हठयोग के प्रमुख ग्रंथों में उन ग्रंथों का समावेश होता है, जो हठयोग के सिद्धांतों, विधियों, और प्रथाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। ये ग्रंथ हठयोग के अनुयायियों और साधकों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। हठयोग के चार प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं:
1. हठयोग प्रदीपिका
- लेखक: स्वामी स्वात्माराम
- काल: 15वीं शताब्दी
- विवरण: यह हठयोग का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें हठयोग की विभिन्न विधियों का विस्तृत वर्णन किया गया है, जैसे कि आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्राएँ, और ध्यान। "हठयोग प्रदीपिका" में कुल 4 अध्याय हैं, जिनमें योग के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। इस ग्रंथ का उद्देश्य हठयोग के माध्यम से साधक को शरीर और मन को नियंत्रित कर आत्म-साक्षात्कार की ओर ले जाना है।
2. गोरक्ष संहिता या गोरक्ष शतक
- लेखक: गुरु गोरखनाथ
- काल: लगभग 10वीं से 11वीं शताब्दी
- विवरण: यह ग्रंथ नाथ संप्रदाय के प्रमुख गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित माना जाता है। इसमें हठयोग के प्रारंभिक सिद्धांतों और साधनाओं का वर्णन किया गया है। गोरक्ष संहिता में शरीर और मन के अनुशासन, योग के साधन, और ध्यान की विधियों पर बल दिया गया है। इसमें योगी के जीवन, साधना, और ध्यान की गहन समझ को स्पष्ट किया गया है।
3. घेरंड संहिता
- लेखक: ऋषि घेरंड
- काल: लगभग 17वीं शताब्दी
- विवरण: घेरंड संहिता हठयोग के शुद्धिकरण और शरीर विज्ञान के पहलुओं पर आधारित है। इसमें हठयोग की 7 अंगों वाली प्रणाली का वर्णन है, जिसे सप्तसाधन कहा जाता है। ये अंग हैं:
1. षट्कर्म (शुद्धिकरण क्रियाएँ)
2. आसन (मुद्राएँ)
3. मुद्रा (ऊर्जा नियंत्रण)
4. प्रत्याहार (इंद्रियों का नियंत्रण)
5. प्राणायाम (श्वास नियंत्रण)
6. ध्यान (ध्यान की विधि)
7. समाधि (आध्यात्मिक एकता)
घेरंड संहिता में हठयोग को "घेरंड समहिता योग" कहा गया है, और इसमें साधक को शरीर और मन की शुद्धि और सामंजस्य की साधना सिखाई जाती है।
4. शिव संहिता
- लेखक: अज्ञात (संभवतः 17वीं शताब्दी)
- विवरण: यह एक अन्य महत्वपूर्ण योग ग्रंथ है, जिसमें हठयोग के साथ-साथ राजयोग और तंत्र साधना का भी समावेश किया गया है। शिव संहिता में शरीर के विभिन्न चक्रों (ऊर्जा केंद्रों), नाड़ियों (ऊर्जा मार्गों), और प्राण (जीवन ऊर्जा) के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। यह ग्रंथ साधक को कुंडलिनी जागरण के मार्ग में सहायता प्रदान करता है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। इसमें योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं का समन्वय है।
अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ
हठयोग के अन्य उल्लेखनीय ग्रंथों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- हठरत्नावली: श्रीनिवास भट्ट द्वारा रचित यह ग्रंथ हठयोग की विभिन्न विधियों और परंपराओं का उल्लेख करता है।
- योगबीज: यह एक छोटा ग्रंथ है, जिसमें हठयोग के तात्विक सिद्धांतों और प्राणायाम की विधियों का वर्णन मिलता है।
हठयोग और आधुनिक युग
आज के समय में हठयोग का अभ्यास पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है। योग के स्वास्थ्य लाभों के कारण यह न केवल भारत में, बल्कि पश्चिमी देशों में भी तेजी से फैल रहा है। हठयोग की शारीरिक मुद्राएँ और प्राणायाम तकनीकें शरीर और मन को स्वस्थ रखने के साथ-साथ मानसिक शांति और ध्यान की अवस्था तक पहुँचने में सहायक होती हैं।
यह सामग्री इंटरनेट के माध्यम से तैयार की गयी है, ज्यादा जानकारी के लिए, उपरोक्त से संबन्धित संस्थान से सम्पर्क करें ।
उपरोक्त सामग्री व्यक्ति विशेष को जानकारी देने के लिए है, किसी समुदाय, धर्म, संप्रदाय की भावनाओं को ठेस या धूमिल करने के लिए नहीं है ।
हमारा उद्देश्य केवल सजगता बढ़ाना है ,हम जन साधारण को संतो, ध्यान विधियों ,ध्यान साधना से संबन्धित पुस्तकों के बारे मे जानकारी , इंटरनेट पर मौजूद सामग्री से जुटाते है । हम किसी धर्म ,संप्रदाय ,जाति , कुल ,या व्यक्ति विशेष की मान मर्यादा को ठेस नही पहुंचाते है । फिर भी जाने अनजाने , यदि किसी को कुछ सामग्री सही प्रतीत नही होती है , कृपया हमें सूचित करें । हम उस जानकारी को हटा देंगे ।
website पर संतो ,ध्यान विधियों , पुस्तकों के बारे मे केवल जानकारी दी गई है , यदि साधकों /पाठकों को ज्यादा जानना है ,तब संबन्धित संस्था ,संस्थान या किताब के लेखक से सम्पर्क करे ।
© 2024. All rights reserved.