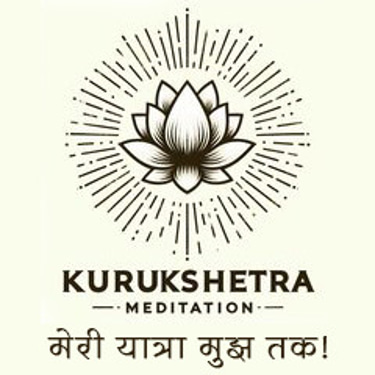“ऋषि और शिष्य की यात्रा”
BLOG
8/18/20251 मिनट पढ़ें
“ऋषि और शिष्य की यात्रा”
एक बार की बात है, एक युवक आरव जीवन की उलझनों से परेशान होकर एक ऋषि के पास पहुँचा। वह शांति और आत्मज्ञान चाहता था। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा –
“पुत्र! आत्मा तक पहुँचने का मार्ग अष्टांग योग है। यदि चाहो तो मैं तुम्हें इसे एक-एक कर सिखाऊँ।”
1. यम – बाहर की दुनिया से संतुलन
पहला दिन – ऋषि ने आरव को जंगल ले जाकर कहा,
“कभी किसी को चोट मत पहुँचाना (अहिंसा), सच बोलना (सत्य), जो तेरा नहीं उसे मत लेना (अस्तेय), अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग मत करना (ब्रह्मचर्य), और लोभ मत करना (अपरिग्रह)।”
आरव ने इन पाँच नियमों का पालन करना शुरू किया और लोगों का विश्वास जीत लिया।
👉 उसका बाहरी जीवन स्वच्छ हुआ।
2. नियम – भीतर की दुनिया से संतुलन
ऋषि ने कहा,
“अब भीतर देखो। शरीर-मन को शुद्ध रखो (शौच), जो है उसी में संतोष रखो (संतोष), कठिनाइयों को सहो (तप), प्रतिदिन आत्मचिंतन करो (स्वाध्याय), और सब कुछ ईश्वर को समर्पित करो (ईश्वर-प्रणिधान)।”
आरव ने यह अभ्यास किया तो उसका मन शांत और निर्मल हो गया।
👉 उसका अंतर्मन शुद्ध हुआ।
3. आसन – शरीर का साधन
एक दिन ऋषि ने कहा –
“लंबे ध्यान के लिए शरीर स्थिर होना चाहिए।”
उन्होंने उसे एक चट्टान पर बैठाकर दिखाया –
“स्थिरसुखमासनम्” – सुखपूर्वक और स्थिर बैठो।
आरव ने कई दिनों तक अभ्यास किया और उसका शरीर रोगमुक्त तथा स्थिर हो गया।
👉 शरीर ध्यान का साथी बना।
4. प्राणायाम – श्वास का विज्ञान
ऋषि बोले –
“श्वास जीवन है। इसे नियंत्रित करना सीखो।”
उन्होंने पूरक, कुम्भक और रेचक सिखाया।
आरव ने पाया कि उसकी बेचैनी कम हो गई और मन गहरा, शांत होने लगा।
👉 प्राण और मन पर अधिकार हुआ।
5. प्रत्याहार – इन्द्रियों को भीतर मोड़ना
ऋषि ने एक दीपक दिखाकर कहा –
“जैसे लौ पर ध्यान देने पर आसपास की अंधकार दिखना बंद हो जाता है, वैसे ही इन्द्रियों को भीतर खींच लो।”
आरव ने अभ्यास किया, अब स्वाद, गंध और शोर उसे विचलित नहीं करते थे।
👉 मन बाहरी आकर्षण से मुक्त होने लगा।
6. धारणा – एकाग्रता
ऋषि ने कहा –
“अब मन को एक बिंदु पर स्थिर करो।”
आरव ने श्वास और मंत्र पर ध्यान केंद्रित किया।
धीरे-धीरे उसका मन चंचलता छोड़कर स्थिर हो गया।
👉 एकाग्रता जन्मी।
7. ध्यान – सतत प्रवाह
धारणा गहरी होकर ध्यान बन गई।
आरव को लगा जैसे उसका मन एक धारा की तरह बह रहा हो, बिना रुकावट, केवल ईश्वर की ओर।
👉 आनंद और शांति की अनुभूति हुई।
8. समाधि – एकत्व
एक रात ध्यान करते-करते आरव खो गया।
ना साधक रहा, ना साधना, केवल शुद्ध चेतना रह गई।
उसे लगा – वह और ईश्वर अलग नहीं, एक ही हैं।
👉 यही समाधि थी।
🌸 निष्कर्ष
ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा –
“देखो पुत्र! यम-नियम से तुमने जीवन को अनुशासित किया, आसन-प्राणायाम से शरीर और प्राण को संतुलित किया, प्रत्याहार-धारणा-ध्यान से मन को शुद्ध किया और अंत में समाधि से आत्मा का मिलन पाया। यही है योग का अष्टांग मार्ग।”
आरव ने प्रणाम किया – उसकी यात्रा अब पूर्ण हो चुकी थी।
"अष्टांग योग"
योग का मूल आधार पतंजलि ऋषि के योगसूत्र में दिया गया है। वहाँ उन्होंने योग का मार्ग "अष्टांग योग" बताया है — यानी योग के आठ अंग। यह आत्म-संयम, शुद्धि और परमात्मा से एकत्व की यात्रा का क्रम है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं:
1. यम (Yama – अनुशासन / संयम)
यम का अर्थ है समाज और अन्य प्राणियों के साथ हमारे व्यवहार पर नियंत्रण।
मुख्य पाँच यम:
अहिंसा – किसी को शारीरिक, मानसिक या वाणी से हानि न पहुँचाना।
सत्य – सत्य बोलना, छल-कपट न करना।
अस्तेय – चोरी न करना, जो हमारा नहीं उसे न लेना।
ब्रह्मचर्य – इन्द्रिय-निग्रह, जीवनशक्ति का सही प्रयोग।
अपरिग्रह – लोभ और संचय की प्रवृत्ति से बचना।
👉 यम से व्यक्ति का बाह्य जीवन शुद्ध होता है।
2. नियम (Niyama – अनुशासन / आत्मसंयम)
ये आंतरिक शुद्धि और आत्म-विकास के नियम हैं।
मुख्य पाँच नियम:
शौच – शारीरिक और मानसिक पवित्रता।
संतोष – जो है उसी में संतोष पाना।
तप – कठिनाइयों को सहते हुए आत्म-संयम का अभ्यास।
स्वाध्याय – आत्मचिंतन, शास्त्र-पठन, मंत्र-जप।
ईश्वर-प्रणिधान – ईश्वर में समर्पण।
👉 नियम से साधक का अंतर्मन शुद्ध होता है।
3. आसन (Asana – स्थिरता)
शरीर को स्थिर और सुखद स्थिति में बैठाना।
इसका उद्देश्य केवल व्यायाम नहीं बल्कि ध्यान के लिए शरीर को स्वस्थ और स्थिर बनाना है।
पतंजलि कहते हैं: "स्थिरसुखमासनम्" – जो आसन स्थिर और सुखद हो वही सही आसन है।
👉 आसन से शरीर रोगमुक्त, लचीला और ध्यान के योग्य बनता है।
4. प्राणायाम (Pranayama – श्वास-नियंत्रण)
"प्राण" यानी जीवनशक्ति, "आयाम" यानी विस्तार।
श्वास को नियंत्रित करके प्राण का संतुलन करना।
चार अंग: पूरक (श्वास लेना), कुम्भक (रोकना), रेचक (श्वास छोड़ना), शून्यक (खाली रखना)।
👉 इससे मन स्थिर होता है, नाड़ी शुद्ध होती हैं, मानसिक बल और एकाग्रता बढ़ती है।
5. प्रत्याहार (Pratyahara – इन्द्रिय-संयम)
इन्द्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना।
जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है।
👉 इससे मन बाहरी विकर्षण से मुक्त होकर साधक की अंतर्दृष्टि विकसित करता है।
6. धारणा (Dharana – एकाग्रता)
मन को किसी एक बिंदु, मंत्र, स्वरूप या श्वास पर केंद्रित करना।
इसका लक्ष्य है मन की चंचलता रोककर उसे एक स्थान पर स्थिर करना।
👉 धारणा से साधक की एकाग्रता और मानसिक शक्ति बढ़ती है।
7. ध्यान (Dhyana – ध्यान / मेडिटेशन)
धारणा का गहन और अखंड रूप।
जब मन निरंतर एक ही धारा में किसी वस्तु या ईश्वर पर प्रवाहित हो, तो उसे ध्यान कहते हैं।
👉 ध्यान से आत्मा की शांति, गहन आनंद और ईश्वर से निकटता का अनुभव होता है।
8. समाधि (Samadhi – परम लय)
ध्यान की अंतिम अवस्था, जहाँ साधक और ध्यान का विषय एक हो जाते हैं।
इसमें अहंकार लुप्त हो जाता है और साधक को आत्मा व परमात्मा का अनुभव होता है।
दो मुख्य प्रकार:
सविकल्प समाधि – जहाँ सूक्ष्म विचार शेष रहते हैं।
निर्विकल्प समाधि – जहाँ कोई भी विचार या भेदभाव नहीं रहता, केवल पूर्ण एकत्व होता है।
👉 यह योग की परम अवस्था है – मोक्ष की ओर ले जाने वाली।
संक्षेप में
यम-नियम = नैतिक अनुशासन
आसन-प्राणायाम = शारीरिक और प्राणिक संतुलन
प्रत्याहार-धारणा-ध्यान = मानसिक अनुशासन और आत्मचिंतन
समाधि = आत्म-साक्षात्कार
हमारा उद्देश्य केवल सजगता बढ़ाना है ,हम जन साधारण को संतो, ध्यान विधियों ,ध्यान साधना से संबन्धित पुस्तकों के बारे मे जानकारी , इंटरनेट पर मौजूद सामग्री से जुटाते है । हम किसी धर्म ,संप्रदाय ,जाति , कुल ,या व्यक्ति विशेष की मान मर्यादा को ठेस नही पहुंचाते है । फिर भी जाने अनजाने , यदि किसी को कुछ सामग्री सही प्रतीत नही होती है , कृपया हमें सूचित करें । हम उस जानकारी को हटा देंगे ।
website पर संतो ,ध्यान विधियों , पुस्तकों के बारे मे केवल जानकारी दी गई है , यदि साधकों /पाठकों को ज्यादा जानना है ,तब संबन्धित संस्था ,संस्थान या किताब के लेखक से सम्पर्क करे ।
© 2024. All rights reserved.