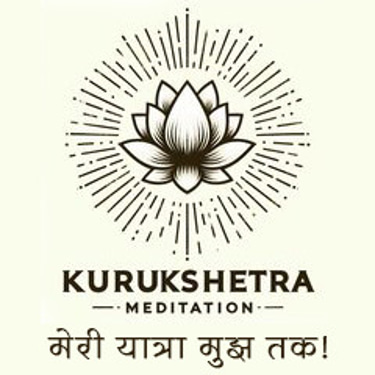समाधि: एक विस्तृत अध्ययन
BLOG
3/23/20251 मिनट पढ़ें
समाधि: एक विस्तृत अध्ययन
संस्कृत में "समाधि" शब्द दो भागों से मिलकर बना है –
"सम" जिसका अर्थ है समान या पूर्ण संतुलन।
"आधि" जिसका अर्थ है ध्यान अथवा स्थिति।
इस प्रकार, समाधि का तात्पर्य मन, बुद्धि और आत्मा की ऐसी अवस्था से है, जिसमें साधक पूर्ण रूप से आत्मचेतना में स्थित हो जाता है और बाहरी संसार से विलग हो जाता है। यह योग का उच्चतम चरण है, जहाँ साधक की चित्तवृत्तियाँ (विचार तरंगें) पूर्ण रूप से शांत हो जाती हैं और वह ब्रह्म (परम सत्य) का साक्षात्कार करता है।
भगवद गीता (6.20-23) में समाधि को उस अवस्था के रूप में वर्णित किया गया है जहाँ योगी आत्मा के भीतर स्थित हो जाता है और परम आनंद का अनुभव करता है।
समाधि के प्रकार
योगशास्त्रों में समाधि को मुख्य रूप से दो वर्गों में बाँटा गया है:
सविकल्प समाधि (Savikalpa Samadhi)
निर्विकल्प समाधि (Nirvikalpa Samadhi)
1. सविकल्प समाधि (Savikalpa Samadhi)
यह समाधि की प्रारंभिक अवस्था होती है, जहाँ साधक अभी भी विचारों से मुक्त नहीं होता, लेकिन वे नियंत्रित होते हैं।
विशेषताएँ:
इसमें साधक अभी भी अपने ध्यान के विषय को देखता या अनुभव करता है।
विचार शांत और नियंत्रित रहते हैं लेकिन पूरी तरह विलीन नहीं होते।
चित्त में "मैं ध्यान कर रहा हूँ" का भाव बना रहता है।
साधक को आत्मज्ञान होता है, लेकिन वह पूर्ण रूप से स्वयं में विलीन नहीं होता।
सविकल्प समाधि के उपप्रकार:
सवितर्क समाधि:
इसमें साधक किसी स्थूल वस्तु या विचार पर ध्यान केंद्रित करता है (जैसे किसी मूर्ति, मंत्र या प्रकाश)।
इसमें विचारों का मंथन चलता रहता है।
निर्वितर्क समाधि:
इसमें साधक किसी वस्तु पर ध्यान करता है, लेकिन उसमें विचारों की कोई व्याख्या नहीं होती।
केवल एकाग्रता होती है, विचार स्वयं समाप्त हो जाते हैं।
सविचार समाधि:
इसमें ध्यान सूक्ष्म स्तर पर होता है, जहाँ व्यक्ति सूक्ष्म तत्वों और ऊर्जाओं का अनुभव करता है।
निर्विचार समाधि:
इसमें सूक्ष्म ध्यान में विचार पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ध्यान के विषय की अनुभूति बनी रहती है।
2. निर्विकल्प समाधि (Nirvikalpa Samadhi)
यह समाधि की उच्चतम अवस्था है, जहाँ साधक सभी विचारों, विकल्पों, और अहंकार से मुक्त होकर पूर्ण ब्रह्म में विलीन हो जाता है।
विशेषताएँ:
इसमें कोई भी मानसिक क्रिया या विचार शेष नहीं रहता।
साधक को अपने शरीर, मन और विचारों का कोई भान नहीं रहता।
पूर्ण रूप से आत्मा और ब्रह्म का एकत्व अनुभव होता है।
यह मोक्ष की अवस्था होती है।
इसमें साधक केवल शुद्ध चेतना में स्थित होता है।
निर्विकल्प समाधि के उपप्रकार:
धर्म मेघ समाधि:
यह समाधि का सर्वोच्च स्तर है, जहाँ साधक ब्रह्म ज्ञान से अभिसिंचित होता है।
इसमें साधक पूर्णत: सत्वगुण में स्थित होता है।
सहज समाधि:
यह अवस्था उन महायोगियों को प्राप्त होती है जो निरंतर समाधि में स्थित रहते हैं, चाहे वे कोई भी कार्य कर रहे हों।
यह जीवन मुक्त अवस्था होती है।
समाधि के अन्य प्रकार
कुछ अन्य योग शास्त्रों में समाधि को और भी श्रेणियों में बाँटा गया है:
संप्रज्ञात समाधि:
इसमें साधक को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन उसकी चेतना अभी भी जागरूक रहती है।
यह सविकल्प समाधि के समान होती है।
असंप्रज्ञात समाधि:
इसमें सभी मानसिक क्रियाएँ समाप्त हो जाती हैं और केवल आत्मा की अनुभूति होती है।
यह निर्विकल्प समाधि के समान होती है।
सहज समाधि:
यह वह अवस्था है जहाँ योगी हर समय समाधि में स्थित रहता है, भले ही वह सामान्य जीवन जी रहा हो।
भाव समाधि:
इसमें साधक पूर्ण प्रेम और भक्ति के साथ ईश्वर में लीन हो जाता है।
भक्तिमार्ग के संत इस समाधि को प्राप्त करते हैं।
जड़ समाधि:
यह ऐसी अवस्था होती है जहाँ व्यक्ति ध्यान में जाने के बाद शरीर से पूर्णतः विच्छिन्न हो जाता है।
कई योगी इसे गुफाओं में साधना के रूप में प्राप्त करते हैं।
समाधि का महत्व
आध्यात्मिक जागरूकता: यह आत्मज्ञान का अंतिम चरण है।
मानसिक शांति: समाधि से मन पूरी तरह शांत हो जाता है।
आनंद और मोक्ष: यह अनंत आनंद और मोक्ष की ओर ले जाती है।
चेतना का विस्तार: समाधि में साधक अपने अस्तित्व से परे जाकर ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव करता है।
निष्कर्ष
समाधि योग की अंतिम अवस्था है, जहाँ साधक आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव करता है। सविकल्प समाधि में अभी भी विचार रहते हैं, जबकि निर्विकल्प समाधि में साधक पूर्ण रूप से ब्रह्म में लीन हो जाता है। समाधि न केवल आत्मज्ञान का साधन है, बल्कि यह मोक्ष प्राप्ति का भी मार्ग है। जो व्यक्ति निरंतर योग और ध्यान का अभ्यास करता है, वह इस दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकता है।
हमारा उद्देश्य केवल सजगता बढ़ाना है ,हम जन साधारण को संतो, ध्यान विधियों ,ध्यान साधना से संबन्धित पुस्तकों के बारे मे जानकारी , इंटरनेट पर मौजूद सामग्री से जुटाते है । हम किसी धर्म ,संप्रदाय ,जाति , कुल ,या व्यक्ति विशेष की मान मर्यादा को ठेस नही पहुंचाते है । फिर भी जाने अनजाने , यदि किसी को कुछ सामग्री सही प्रतीत नही होती है , कृपया हमें सूचित करें । हम उस जानकारी को हटा देंगे ।
website पर संतो ,ध्यान विधियों , पुस्तकों के बारे मे केवल जानकारी दी गई है , यदि साधकों /पाठकों को ज्यादा जानना है ,तब संबन्धित संस्था ,संस्थान या किताब के लेखक से सम्पर्क करे ।
© 2024. All rights reserved.