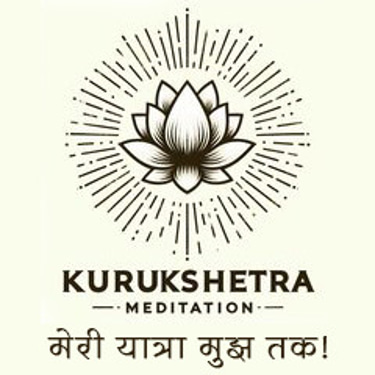संत कबीर दास
कबीरा
SAINTS
10/21/20241 मिनट पढ़ें
संत कबीर दास
मध्य युगीन भारत के एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से भक्ति आंदोलन को महत्वपूर्ण दिशा दी। वे निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत माने जाते हैं। कबीर का जीवन सरल, सच्चा और ईश्वर भक्ति से प्रेरित था। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से प्रेम, सद्भाव और सामाजिक समानता का संदेश दिया। कबीर का जीवन और उनके विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणादायक हैं।
जन्म और प्रारंभिक जीवन:
कबीर का जन्म 1398 ई. के आस-पास हुआ था। उनके जन्म के बारे में कई मतभेद हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार, वे काशी (वर्तमान बनारस) में जन्मे थे और उनका पालन-पोषण नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति ने किया था, जो मुस्लिम थे। उनके जन्म के बारे में एक प्रसिद्ध लोककथा यह है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, जिसने लोकलाज के भय से उन्हें त्याग दिया। नीरू और नीमा ने उन्हें अपनाया और उनका पालन-पोषण किया।
शिक्षा और आध्यात्मिकता:
कबीर को पारंपरिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन उनका ज्ञान और अनुभव बहुत गहन था। कहा जाता है कि कबीर ने गुरू रामानंद से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी। एक कथा के अनुसार, कबीर ने रामानंद को गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए गंगा किनारे उनकी राह में लेट गए थे, जिससे रामानंद का पांव उनके शरीर से छू गया और उन्होंने "राम-राम" कहा। इसे कबीर ने गुरु मंत्र के रूप में स्वीकार किया और राम नाम की भक्ति में लीन हो गए।
कबीर ने वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, लेकिन उनके विचार गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक थे। वे अपने विचारों को आम जनता की भाषा में व्यक्त करते थे, जिससे वे समाज के सभी वर्गों में लोकप्रिय हो गए।
भक्ति और विचारधारा:
कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वे ईश्वर को निराकार, अद्वितीय और सर्वव्यापी मानते थे। उनका मानना था कि ईश्वर को पाने के लिए किसी मूर्ति, मंदिर, मस्जिद, या विशेष धार्मिक कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति केवल सच्चे हृदय, प्रेम और भक्ति से की जा सकती है। उनके प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं:
1. निर्गुण भक्ति: कबीर ने निराकार भगवान की उपासना की। उन्होंने मूर्तिपूजा, कर्मकांड और पाखंड का विरोध किया और सीधे ईश्वर से जुड़ने पर जोर दिया।
2. सामाजिक समानता: कबीर जाति-व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य समान हैं और जाति, धर्म, या जन्म के आधार पर किसी को ऊँचा या नीचा नहीं माना जाना चाहिए।
3. धार्मिक एकता: कबीर ने हिंदू-मुस्लिम एकता का संदेश दिया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धार्मिक परंपराओं में व्याप्त आडंबर और कट्टरता का विरोध किया। उनके अनुसार, ईश्वर न तो हिंदू है, न मुस्लिम, बल्कि वह हर व्यक्ति में वास करता है।
4. सत्य की महत्ता: कबीर ने सत्य को सर्वोच्च महत्व दिया। उन्होंने जीवन में सच्चाई, सरलता और ईमानदारी पर जोर दिया। उनके अनुसार, व्यक्ति को अपने आचरण में सत्यनिष्ठ होना चाहिए।
5. प्रेम का संदेश: कबीर के अनुसार, प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को सभी प्राणियों से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर प्रत्येक जीव में वास करता है।
साहित्य और रचनाएं:
कबीर की वाणी लोकभाषा में सरल और सीधी होती थी, जिससे आम जनता उनकी बातों को आसानी से समझ सके। उन्होंने "साखी", "सबद" और "रमैनी" के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। उनकी रचनाओं में गहरी भक्ति, दार्शनिक विचार और समाज सुधार का संदेश मिलता है। उनके दोहे अत्यधिक प्रसिद्ध हैं और उनमें जीवन के गहन सत्य सरल शब्दों में प्रस्तुत किए गए हैं। कबीरदास की प्रमुख रचनाएँ इस प्रकार हैं:
1. साखी (कहावतें या दोहे)
कबीर की साखियाँ (अर्थात् संक्षिप्त कविताएँ) उनके जीवन और दर्शन का सार प्रस्तुत करती हैं। इन साखियों के माध्यम से उन्होंने जीवन के गहरे सत्य, ईश्वर की भक्ति, और सामाजिक सुधार के विचारों को प्रस्तुत किया। ये साखियाँ दो पंक्तियों में व्यक्त होती हैं, जिन्हें "दोहे" कहा जाता है। साखियों में कबीर ने ईश्वर की उपासना के महत्व, सांसारिक माया से मुक्त होने की सलाह, और सच्ची भक्ति का मार्ग बताया है। उन्होंने धार्मिक कट्टरता, मूर्तिपूजा, और पाखंड पर तीखा प्रहार किया है।
1. "बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय"
- इसमें कबीर आत्मनिरीक्षण की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जब वे दूसरों में बुराई ढूंढने निकले, तो उन्हें कोई बुरा नहीं मिला, लेकिन जब उन्होंने अपने भीतर देखा, तो पाया कि वे स्वयं से बुरे कोई नहीं हैं। यह दोहा हमें आत्ममूल्यांकन और विनम्रता का पाठ सिखाता है।
2. "दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय"
- इस दोहे में कबीर ने मानव स्वभाव पर कटाक्ष किया है कि लोग केवल दुख के समय ही भगवान को याद करते हैं। यदि वे सुख के समय में भी भगवान का स्मरण करें, तो जीवन में दुख की स्थिति ही नहीं आएगी। यह रचना स्थायी भक्ति और निष्ठा का संदेश देती है।
3. "संत ना छाड़ै संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग।"
इस दोहे में कबीर समझाते हैं कि एक सच्चा संत अपनी संतई (साधुता) नहीं छोड़ता, चाहे उसे लाखों असंत (असभ्य व्यक्ति) मिल जाएं। जैसे चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उसका शीतल प्रभाव और सुगंध बरकरार रहती है। इसी प्रकार, एक सच्चे संत पर नकारात्मकता का कोई असर नहीं होता। यह दोहा सच्चाई, शांति और अच्छाई के महत्व को दर्शाता है।
4. "पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।"
कबीर कहते हैं कि बहुत सारे शास्त्र पढ़ने के बावजूद कोई पंडित (ज्ञानी) नहीं बनता। असली ज्ञान "प्रेम" के ढाई अक्षरों में है। जो प्रेम का सही अर्थ समझ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी या पंडित होता है। यह दोहा जीवन में प्रेम और करुणा के महत्व को बताता है, और बाहरी ज्ञान से ज्यादा आंतरिक अनुभूति को महत्व देता है।
5. "माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। कर का मनका डार दे, मन का मनका फेर।"
कबीर इस दोहे में कहते हैं कि माला (प्रार्थना की माला) फेरने में व्यक्ति का पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन उसके मन का फेर (विचारों की अशुद्धता) नहीं बदलता। इसका समाधान यह है कि बाहरी कर्मकांडों को छोड़कर अपने मन के विचारों को शुद्ध किया जाए। इसका तात्पर्य यह है कि सच्ची भक्ति और ध्यान केवल बाहरी कर्मकांडों से नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता से होती है।
6. "तिनका कबहुँ न निंदिये, जो पाँवन तर होय। कबहुँ उड़ आँखिन पड़े, तो पीर घनेरी होय।"
इस दोहे में कबीर कहते हैं कि हमें कभी भी छोटे से छोटे व्यक्ति या चीज़ की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो तिनका पाँव के नीचे होता है, वही कभी आँख में गिरकर हमें कष्ट पहुंचा सकता है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति या चीज़ का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कब हमें प्रभावित कर सकता है, यह कहा नहीं जा सकता।
7. "कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढे बन माहि। ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाहि।"
कबीर इस दोहे में एक मृग (हिरण) के माध्यम से समझाते हैं कि जैसे कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन वह उसे जंगल में ढूंढता फिरता है, वैसे ही भगवान हमारे भीतर हैं, लेकिन हम उन्हें बाहर ढूंढते रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर को पाने के लिए हमें अपने भीतर झाँकने की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर हमारे हृदय में ही निवास करते हैं।
8. "रात गंवाई सोय कर, दिवस गंवाया खाय। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाय।"
इस दोहे में कबीर कहते हैं कि हम रात को सोने में और दिन को खाने में बिता देते हैं। हमारा जन्म हीरे के समान अनमोल था, लेकिन हम इसे तुच्छ कौड़ी के बदले गवां देते हैं। यह दोहा जीवन की नश्वरता और उसके सही उपयोग की आवश्यकता पर बल देता है। कबीर का कहना है कि हमें अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति और सही कार्यों में लगाना चाहिए।
9. "कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर।"
कबीर इस दोहे में कहते हैं कि वे लोग अंधे (मूर्ख) हैं जो गुरु को साधारण मानते हैं। यदि भगवान नाराज हो जाएं, तो गुरु हमें सहारा दे सकते हैं, लेकिन यदि गुरु नाराज हो जाएं, तो कोई सहारा नहीं होता। यह दोहा गुरु के महत्व और उनके प्रति सच्ची श्रद्धा को दर्शाता है।
10. "साईं इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाय। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाय।"
कबीर इस दोहे में एक संतुलित जीवन की प्रार्थना कर रहे हैं। वे भगवान से निवेदन करते हैं कि उन्हें उतना ही दिया जाए, जिससे वे अपने परिवार का पालन कर सकें और जरूरतमंद साधुओं को भी भोजन दे सकें। यह दोहा मध्यमार्ग का संदेश देता है कि हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिए और दूसरों की भी सहायता करनी चाहिए।
2. सबद (भजन या गीत)
सबद कबीर की भक्ति रचनाएँ हैं, जिनमें उन्होंने ईश्वर के प्रति अपने गहरे प्रेम और भक्ति को व्यक्त किया है। ये सबद गीतों या भजनों के रूप में होते हैं, जो कबीर के आध्यात्मिक अनुभव और भक्ति के मार्ग की ओर इशारा करते हैं। इन रचनाओं में उन्होंने अपने निर्गुण ब्रह्म के प्रति प्रेम और ध्यान की महत्ता को प्रकट किया है। सबदों में कबीर ने ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी माना है और सीधे ईश्वर की उपासना की बात की है।
1. सबद का आध्यात्मिक अर्थ:
कबीरदास के सबद में ईश्वर को पाने का मार्ग और आत्मा के सत्य को समझने का प्रयास किया गया है। कबीर के अनुसार, ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को आत्मज्ञान की आवश्यकता है, जो केवल शब्द (सबद) के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। इस सबद का गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है, जो व्यक्ति के भीतर के सत्य को प्रकट करता है और उसे बाहरी मोह-माया से मुक्त करता है।
"सतगुरु की महिमा अगम अपारा, कौन जाने बिन शब्द विचारा।"
इस सबद में कबीर कहते हैं कि सतगुरु की महिमा को बिना शब्द (आत्मज्ञान या भक्ति के शब्द) के नहीं समझा जा सकता। यहां शब्द का मतलब गुरु की वाणी से है, जो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। यह हमें अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है और ईश्वर की ओर मार्ग दिखाती है।
2. सच्चे गुरु और सबद की महिमा:
कबीरदास ने गुरु की महत्ता को अपने सबद में बार-बार उल्लेखित किया है। उनके अनुसार, सच्चे गुरु ही वो होते हैं, जो सबद के माध्यम से आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। सबद में गुरु की वाणी को सुनकर व्यक्ति अपने अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकलता है और ईश्वर की ओर अग्रसर होता है।
"साधो, यह तन थाथ न होई, पाय जमालि चले पतंग। शब्द न चीन्हा आपना, गुरु गम्भीर अनंग।"
कबीर इस सबद में यह कहते हैं कि शरीर का अंत निश्चित है और इस मरणशील शरीर को लेकर चलने से कोई लाभ नहीं है। जिन्होंने अपने भीतर के सबद को नहीं पहचाना, वे जीवन के सत्य को नहीं समझ पाएंगे। गुरु का सबद ही हमें इस शरीर के असारता का ज्ञान कराता है और आत्मा के सत्य का मार्ग दिखाता है।
3. निर्गुण ब्रह्म की भक्ति और सबद का संदेश:
कबीर के सबद में निर्गुण भक्ति का विशेष महत्व है। निर्गुण भक्ति वह है, जिसमें ईश्वर को निराकार, अव्यक्त और सर्वव्यापी माना जाता है। कबीर ने सबद के माध्यम से कहा है कि ईश्वर को न तो देखा जा सकता है और न ही उसकी कोई मूर्ति बनाई जा सकती है। वे कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार केवल सबद के माध्यम से किया जा सकता है, जब मनुष्य अपने मन और आत्मा को शुद्ध करता है।
"झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे कै ताना काहे कै भरनी।"
यह सबद आत्मा और शरीर के संबंध को बताता है। कबीर कहते हैं कि हमारे शरीर को ईश्वर ने बड़ी बारीकी से बुनकर तैयार किया है, लेकिन यह शरीर अस्थायी है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है, वह मोह-माया से मुक्त होकर आत्मा की सच्ची पहचान करता है। सबद के माध्यम से ही यह गहन बोध होता है।
4. माया और संसार की असारता:
कबीरदास के सबद में माया, मोह, और संसारिक सुखों को नकारा गया है। उनके अनुसार, संसार केवल एक नाटक है और इसकी असारता को समझने के बाद ही व्यक्ति सच्ची भक्ति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। कबीर ने सबद के माध्यम से बार-बार यह समझाया है कि इस संसार के आकर्षण से मुक्त होकर ईश्वर की शरण में जाना ही वास्तविक जीवन का उद्देश्य है।
"माया मरी न मन मरा, मर मर गये शरीर। आसा त्रिस्ना ना मरी, कह गए दास कबीर।"
इस सबद में कबीर ने माया और इच्छाओं की व्यर्थता को बताया है। वे कहते हैं कि शरीर मर सकता है, लेकिन जब तक मन और इच्छाएं जीवित हैं, तब तक आत्मा का मोक्ष संभव नहीं है। माया से मुक्त होने का संदेश कबीर के सबदों का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
5. सबद के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का मिलन:
कबीरदास के अनुसार, सबद ही वह माध्यम है जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। कबीर के सबद में बताया गया है कि जब व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज़ (सबद) सुनता है, तब वह ईश्वर के निकट पहुंचता है। यह एक गहरा आत्मिक अनुभव है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है।
"हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या।"
इस सबद में कबीर ने बताया कि जब व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, तब उसे संसार की कोई चिंता नहीं रहती। उसकी आत्मा इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है कि वह केवल ईश्वर के प्रेम में मस्त हो जाता है। इस स्थिति में सबद ही उसका मार्गदर्शक होता है, जिससे वह संसार के बंधनों से मुक्त होता है।
6. समाज सुधार और सबद के संदेश:
कबीर के सबद समाज सुधार के संदेश भी देते हैं। उन्होंने धार्मिक पाखंड, जाति-व्यवस्था, और सामाजिक कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। उनके सबद समाज में फैली असमानताओं और धार्मिक आडंबरों के खिलाफ एक तीखा विरोध प्रकट करते हैं। कबीर ने अपने सबदों के माध्यम से सच्ची भक्ति और समभाव का प्रचार किया, जिसमें कोई जाति, धर्म, या वर्ग का भेदभाव नहीं है।
"कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।"
इस सबद में कबीर समाज के हर व्यक्ति के लिए शुभकामनाएँ मांगते हैं। वे कहते हैं कि न तो किसी से दोस्ती होनी चाहिए, न ही किसी से शत्रुता। यह समभाव और समदृष्टि का प्रतीक है, जो कबीर के समाज सुधार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है।
3. रमैनी
कबीर की रमैनी एक प्रकार की गद्यात्मक कविता है, जिसमें उन्होंने आध्यात्मिक अनुभवों और भक्ति के मार्ग को विस्तार से समझाया है। रमैनी में कबीर ने व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा दी है और संसार की असारता को उजागर किया है। इन रचनाओं में भक्ति, ध्यान और मोक्ष के विषयों पर गहरा चिंतन किया गया है।
1. भक्ति का मार्ग: कबीर की रमैनी में भक्ति को सर्वोपरि माना गया है। वे संसारिक भोग-विलास, धन-संपत्ति, और मोह-माया को तुच्छ बताते हैं और कहते हैं कि सच्चा सुख और शांति केवल भगवान की भक्ति में है। रमैनी के माध्यम से कबीर ने यह बताया है कि भगवान की प्राप्ति बाहरी साधनों या आडंबरों से नहीं होती, बल्कि सच्ची निष्ठा और प्रेम से होती है।
"रमैनी राम रतन धन पायो"
इसमें कबीर कहते हैं कि राम का नाम (ईश्वर) सबसे बड़ा धन है, और जिसने इसे प्राप्त कर लिया, वह संसार के सभी दुखों से मुक्त हो गया। इस रमैनी में कबीर यह समझाते हैं कि ईश्वर की भक्ति और उनके नाम की महिमा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सांसारिक धन-संपत्ति अस्थायी है, लेकिन भगवान की भक्ति अमूल्य है और इससे जीवन को सार्थकता मिलती है।
2. ज्ञान और आत्मा का बोध:
कबीर की रमैनी में आत्मज्ञान और ईश्वर के साथ आत्मा के संबंध पर गहन चिंतन किया गया है। कबीर ने रमैनी के माध्यम से यह संदेश दिया कि हमें अपने भीतर झाँकने और आत्मा के सत्य को समझने की आवश्यकता है। ईश्वर हमारे भीतर ही हैं, और हमें उन्हें बाहर खोजने की बजाय अपने मन के भीतर देखना चाहिए।
"घट घट में पंछी बोलता, चढ़ि उतरै दिन रैन।
आसा माया मोह में, फंदि रह्यो आन्हैं।"
कबीर इस रमैनी में समझाते हैं कि हर जीव के भीतर एक दिव्य तत्व (ईश्वर) विद्यमान है, लेकिन लोग माया, मोह, और इच्छाओं के बंधन में बंधे हुए हैं, जिससे वे इस सत्य को नहीं देख पाते। वे कहते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य इस बंधन से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करना है।
3. निर्गुण भक्ति और पाखंड का विरोध:
कबीर की रमैनी में निर्गुण भक्ति का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। वे ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी मानते थे और मूर्तिपूजा तथा कर्मकांडों का विरोध करते थे। रमैनी में कबीर ने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि ईश्वर को मंदिर, मस्जिद या अन्य धार्मिक स्थलों में ढूंढने की बजाय, हमें उन्हें अपने हृदय में महसूस करना चाहिए।
"मोको कहां ढूंढे रे बन्दे, मैं तो तेरे पास में"
इस रमैनी में कबीर ने बताया कि ईश्वर को बाहर ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वे हर किसी के भीतर रहते हैं। यह रमैनी पाखंड, आडंबर और बाहरी साधनों से ईश्वर को पाने की कोशिशों का विरोध करती है और सच्ची भक्ति को ही सबसे महत्वपूर्ण बताती है।
4. संसार की नश्वरता और माया का बंधन:
कबीर की रमैनी में संसार को एक असार और नश्वर स्थान बताया गया है, जहाँ माया और मोह के बंधन में बंधकर इंसान अपनी आत्मा के सत्य को भूल जाता है। उन्होंने रमैनी के माध्यम से यह संदेश दिया कि संसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर ही आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।
"माया मरी न मन मरा, मर मर गये शरीर। आसा त्रिस्ना ना मरी, कह गए दास कबीर।"
इस रमैनी में कबीर कहते हैं कि शरीर तो नश्वर है और एक दिन यह समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि माया और इच्छाओं का त्याग नहीं किया गया, तो आत्मा का मोक्ष संभव नहीं है। यह रचना माया और मोह के बंधनों से मुक्ति की आवश्यकता पर जोर देती है।
5. जीवन और मृत्यु का बोध:
कबीर की रमैनी में जीवन और मृत्यु को एक प्राकृतिक सत्य के रूप में देखा गया है। कबीर कहते हैं कि हमें मृत्यु से डरने की बजाय इसे आत्मज्ञान के मार्ग में एक मोड़ के रूप में देखना चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता।
"जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। कब मरहूँ कब पाईअ, पूर्ण परमानंद।"
इस रमैनी में कबीर ने मृत्यु का स्वागत किया है। वे कहते हैं कि जिस मृत्यु से संसार डरता है, उसी से उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि उनके लिए मृत्यु के बाद ईश्वर के साथ मिलन का अवसर होता है।
6. ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग:
कबीर की रमैनी में ईश्वर की प्राप्ति का सरल मार्ग बताया गया है। कबीर ने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी विशेष कर्मकांड, व्रत, या तप की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति, आत्मज्ञान और सदाचरण ही पर्याप्त हैं। वे सांसारिक माया-मोह को छोड़कर साधना और ध्यान पर जोर देते हैं।
"नाम जपो जी नाम जपो, सद्गुरु भेद बताय। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हरि से लागे जाय।"
इस रमैनी में कबीर ने ईश्वर के नाम का जप करने की महत्ता बताई है। उनका कहना है कि जो साधक सच्चे मन से ईश्वर के नाम का स्मरण करता है, उसे ईश्वर की कृपा अवश्य मिलती है। यह रमैनी ईश्वर की भक्ति की शक्ति को प्रकट करती है और साधकों को नाम स्मरण की सलाह देती है।
कबीर बीजक- संत कबीरदास की एक महत्वपूर्ण काव्य रचना है, जो उनकी भक्ति, ज्ञान, और समाज सुधार के विचारों को समाहित करती है। "बीजक" शब्द का अर्थ "बीज" होता है, और इसे कबीरदास की रचनाओं का सार कहा जा सकता है। बीजक को कबीरदास के अनुयायियों द्वारा विभिन्न विधाओं में गाया जाता है और इसे उनकी काव्य परंपरा में विशेष स्थान प्राप्त है।
कबीर बीजक की संरचना
कबीर बीजक मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित है:
1. साखी: ये कबीर के विचारों का संक्षिप्त और सारगर्भित रूप हैं। साखियों में कबीर ने गहन ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत किया है।
2. रमैनी: रमैनी में कबीर ने भक्ति, समाजिक समस्याओं और जीवन के गहरे अर्थों का विवेचन किया है। यह गीतात्मक रूप में होती है और भक्ति संगीत में गाई जाती है।
3. सबद: सबद में कबीर ने ईश्वर, आत्मा और ब्रह्म के संबंध को समझाने का प्रयास किया है। यह रूप में गहन और दार्शनिक विचार होते हैं।
कबीर बीजक के मुख्य तत्व
1. निर्गुण भक्ति: कबीर ने बीजक में निर्गुण भक्ति का प्रतिपादन किया है। उन्होंने ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी माना है और मूर्तिपूजा का विरोध किया है। उनका मानना है कि ईश्वर का अनुभव केवल अंतर्मन की शुद्धता से किया जा सकता है।
2. समाज सुधार: कबीर बीजक में समाज में फैली कुरीतियों और जातिवाद का कड़ा विरोध किया गया है। उन्होंने भक्ति को एक साधारण और समभाव का माध्यम बताया है, जिसमें किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का भेदभाव नहीं है।
3. आध्यात्मिक अनुभव: बीजक में कबीर ने अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभवों को साझा किया है। उनके शब्दों में गहरा अनुभव और सत्यता है, जो पाठकों को आत्मा के वास्तविक स्वरूप की पहचान कराने का प्रयास करती है।
4. माया और मोह का त्याग: कबीर ने माया, मोह, और सांसारिक इच्छाओं को त्यागने की बात की है। उन्होंने बताया कि केवल आत्मज्ञान और भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है।
5. प्रेम और करुणा: कबीर के बीजक में प्रेम और करुणा का महत्व भी दर्शाया गया है। वे मानते हैं कि सच्ची भक्ति प्रेम और करुणा के बिना अधूरी है।
कबीर बीजक के प्रमुख उद्धरण
कबीर बीजक में कई प्रसिद्ध साखियाँ और रमैनी हैं, जो गहरे अर्थ और शिक्षाएं देती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख उद्धरण दिए गए हैं:
1. "बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय।
जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय।"
इस साखी में कबीर आत्ममूल्यांकन का संदेश देते हैं।
2. "साईं इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाय।
मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाय।"
यह रमैनी सादगी और परोपकार के महत्व को दर्शाती है।
3. "कबीर, मन के मीत हैं, दुनिया के मीत नहीं।
जो मन में हरि बसे हैं, वही मीत सच्चा।"
यहाँ कबीर यह बताते हैं कि सच्चा मित्र वही है, जो मन में भगवान की उपस्थिति को महसूस करता है।
4. "साधो, यह तन थाथ न होई, पाय जमालि चले पतंग।
शब्द न चीन्हा आपना, गुरु गम्भीर अनंग।"
इस साखी में कबीर कहते हैं कि हमारे शरीर का अंत निश्चित है, और सच्चे गुरु की वाणी ही हमें आत्मा के सत्य को समझाती है।
कबीर बीजक का महत्व
कबीर बीजक भारतीय भक्ति साहित्य में एक अनमोल रत्न है। इसकी रचनाएँ आज भी भक्ति, ज्ञान, और आत्मा के साधकों के लिए प्रेरणास्रोत बनी हुई हैं। कबीर के विचारों में गहनता और सामयिकता है, जो सभी समयों में प्रासंगिक बने रहते हैं।
कबीर बीजक का अध्ययन न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज के प्रति संवेदनशीलता, प्रेम, करुणा, और सामाजिक न्याय के लिए भी एक मार्गदर्शक है। इसके द्वारा हम एक बेहतर समाज की रचना की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं।
समाज सुधारक के रूप में योगदान:
कबीर केवल एक संत ही नहीं, बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड, धार्मिक कट्टरता और जातिगत भेदभाव का विरोध किया। उनके अनुसार, ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधारण और सच्ची भक्ति पर्याप्त है, और किसी विशेष कर्मकांड या जाति का कोई महत्व नहीं है।
उन्होंने न केवल धार्मिक विभाजन को समाप्त करने का प्रयास किया, बल्कि समाज में समानता और भाईचारे की भावना को भी प्रोत्साहित किया। कबीर ने अपने समय के सामाजिक और धार्मिक भेदभाव का कड़ा विरोध किया और एक नए आध्यात्मिक मार्ग की स्थापना की, जो प्रेम, करुणा और समानता पर आधारित था।
संत कबीरदास की रचनाएँ उनके जीवन, विचार और भक्ति के गहन दृष्टिकोण का प्रतिबिंब हैं। उनकी काव्य रचनाएँ सरल, सारगर्भित और जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती हैं। कबीर ने अपने काव्य में सामाजिक सुधार, ईश्वर की भक्ति, धार्मिक आडंबरों का विरोध और प्रेम का संदेश दिया है। उनकी भाषा आम बोलचाल की थी, जो आसानी से सभी के लिए समझने योग्य थी। उनके द्वारा रचित साखियाँ, सबद, रमैनी और अन्य काव्य रूपों में उनके गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक विचार स्पष्ट होते हैं।
4. अन्य रचनाएँ
कबीर की अन्य रचनाओं में भी उनके सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण का वर्णन मिलता है। उनकी भाषा में सादगी थी, जो आम जनमानस तक सीधे पहुँचती थी। उनके पद, साखियाँ और भजन आम जीवन की सच्चाइयों और भक्ति के रास्ते को सरलता से बताते हैं। कबीर की रचनाओं में कई जगहों पर हिंदू-मुस्लिम एकता का संदेश दिया गया है और धर्म के नाम पर हो रही बर्बरता और कट्टरता का विरोध किया गया है।
5. कबीर का साहित्य और उसकी भाषा -कबीर ने अवधी, ब्रज और खड़ी बोली जैसी भाषाओं में अपनी रचनाएँ कीं। उनकी भाषा में सादगी, व्यावहारिकता और आम बोलचाल की शैली है, जिसे हर वर्ग का व्यक्ति समझ सकता है। उनके दोहों में न केवल भक्ति का संदेश होता है, बल्कि जीवन के गहरे दर्शन और समाज सुधार की बातें भी मिलती हैं। वे समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जातिवाद और पाखंड का विरोध करते थे और उनके दोहे इन सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार करते हैं।
कबीर के साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ:
1. सादगी: कबीर की भाषा सरल और सुलभ थी। वे कठिन शब्दों और जटिल विचारों से परे जाकर सीधे जीवन के मूलभूत तथ्यों को व्यक्त करते थे।
2. व्यावहारिकता: कबीर का काव्य व्यावहारिक जीवन पर आधारित है। उन्होंने अपने अनुभवों और समाज के यथार्थ पर आधारित काव्य लिखा।
3. समाज सुधार: कबीर का साहित्य जाति, धर्म, और सामाजिक असमानता के खिलाफ था। वे जातिवाद और धार्मिक पाखंडों का खुलकर विरोध करते थे।
4. भक्ति और प्रेम: कबीर का काव्य भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण है। उन्होंने ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया और इसे ही मोक्ष का मार्ग माना।
मृत्यु:
कबीर की मृत्यु के समय भी उनके जीवन की तरह विवाद रहा। कहा जाता है कि 1518 ईस्वी में उनका निधन हुआ। एक कथा के अनुसार, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके हिंदू और मुस्लिम अनुयायियों में उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हो गया। हिंदू उन्हें जलाना चाहते थे और मुस्लिम उन्हें दफनाना चाहते थे। किंवदंती है कि जब उन्होंने कबीर के शव पर से चादर हटाई, तो वहां केवल फूल मिले। इन फूलों को आधा हिंदू और आधा मुस्लिम अनुयायियों ने बांट लिया और अपने-अपने रीति-रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार किया। यह घटना कबीर के विचारों की सजीव मिसाल है कि ईश्वर किसी विशेष धर्म, जाति, या पंथ में बंधा नहीं है।
संत कबीर का जीवन समाज के लिए एक अद्वितीय उदाहरण है। उनके विचारों ने न केवल भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी, बल्कि समाज में समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश भी फैलाया। उनके दोहे और भजन आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कबीर का जीवन और उनके उपदेश सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लोगों के लिए प्रासंगिक हैं, और उनका संदेश प्रेम, सत्य, और मानवता का सबसे बड़ा प्रतीक है।
यह सामग्री इंटरनेट के माध्यम से तैयार की गयी है, ज्यादा जानकारी के लिए, उपरोक्त से संबन्धित संस्थान से सम्पर्क करें ।
उपरोक्त सामग्री व्यक्ति विशेष को जानकारी देने के लिए है, किसी समुदाय, धर्म, संप्रदाय की भावनाओं को ठेस या धूमिल करने के लिए नहीं है ।
हमारा उद्देश्य केवल सजगता बढ़ाना है ,हम जन साधारण को संतो, ध्यान विधियों ,ध्यान साधना से संबन्धित पुस्तकों के बारे मे जानकारी , इंटरनेट पर मौजूद सामग्री से जुटाते है । हम किसी धर्म ,संप्रदाय ,जाति , कुल ,या व्यक्ति विशेष की मान मर्यादा को ठेस नही पहुंचाते है । फिर भी जाने अनजाने , यदि किसी को कुछ सामग्री सही प्रतीत नही होती है , कृपया हमें सूचित करें । हम उस जानकारी को हटा देंगे ।
website पर संतो ,ध्यान विधियों , पुस्तकों के बारे मे केवल जानकारी दी गई है , यदि साधकों /पाठकों को ज्यादा जानना है ,तब संबन्धित संस्था ,संस्थान या किताब के लेखक से सम्पर्क करे ।
© 2024. All rights reserved.