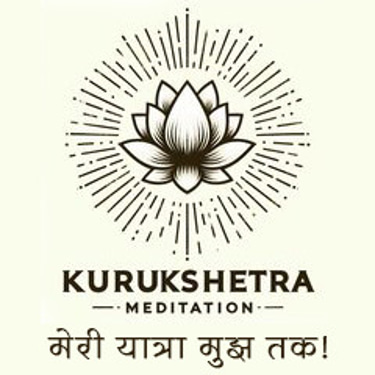अभिनवभारती
"अभिनवगुप्त"
BLOG
12/4/20241 मिनट पढ़ें
अभिनवभारती -अभिनवगुप्त
अभिनवभारती अभिनवगुप्त की एक महत्वपूर्ण कृति है, जो भारतीय काव्यशास्त्र और रस सिद्धांत पर आधारित है। यह ग्रंथ आचार्य भरतमुनि के नाट्यशास्त्र पर लिखी गई एक व्यापक और गहन टीका है। इसे काव्यशास्त्र और नाट्यकला पर आधारित भारतीय परंपरा की सबसे समृद्ध व्याख्या माना जाता है। अभिनवभारती ने भारतीय साहित्य, नाटक, और सौंदर्यशास्त्र के अध्ययन में एक अमूल्य योगदान दिया है।
अभिनवभारती का परिचय
लेखक:
अभिनवभारती को कश्मीर शैव दर्शन के महान आचार्य अभिनवगुप्त ने लिखा।
प्रमुख विषय:
यह ग्रंथ मुख्य रूप से नाट्यशास्त्र के रस सिद्धांत, नाट्य कला, और काव्यशास्त्र के गूढ़ सिद्धांतों की व्याख्या करता है।
इसमें नाट्यशास्त्र के हर अध्याय की विस्तार से व्याख्या की गई है।
लेखन का उद्देश्य:
भारतीय काव्य और नाट्य परंपरा के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट करना।
नाट्य और काव्य को दार्शनिक दृष्टिकोण से जोड़कर समझाना।
रस सिद्धांत को सार्वभौमिक और जीवन के अनुभवों से जोड़ना।
महत्व:
अभिनवभारती काव्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र पर आज तक का सबसे प्रभावशाली टीका ग्रंथ है।
यह भारतीय सौंदर्यशास्त्र के अध्ययन के लिए एक आधारशिला के रूप में कार्य करता है।
अभिनवभारती में प्रमुख विषय
1. रस सिद्धांत की व्याख्या
अभिनवगुप्त ने रस सिद्धांत को नाट्यशास्त्र से लेकर और अधिक दार्शनिक ऊँचाई पर पहुँचा दिया।
उन्होंने "रस" को केवल नाटकीय आनंद न मानकर, इसे आध्यात्मिक अनुभव से जोड़ा।
उन्होंने भरतमुनि के "रस सूत्र" —
"विभावानुभावव्याभिचारि संयोगाद्रसनिष्पत्तिः"
की व्याख्या करते हुए बताया कि रस का अनुभव कैसे होता है।रस के आठ प्रकार:
अभिनवभारती में नाट्यशास्त्र में वर्णित आठ रसों (श्रृंगार, वीर, करुण, अद्भुत, रौद्र, हास्य, भयानक, और वीभत्स) की विस्तार से चर्चा की गई है।शांत रस का समावेश:
अभिनवगुप्त ने शांत रस को नौवाँ रस माना और इसे सभी रसों का चरम रूप बताया। उनके अनुसार, शांत रस में ही आत्मा के आनंद की परिपूर्णता होती है।
2. साधारणीकरण (Universalization)
अभिनवगुप्त ने साधारणीकरण की अवधारणा को विस्तार से समझाया।
साधारणीकरण का अर्थ है कि नाटक या काव्य में जो भावनाएँ और अनुभव व्यक्त किए जाते हैं, वे व्यक्तिगत न रहकर सार्वभौमिक बन जाते हैं।
यह प्रक्रिया दर्शकों या पाठकों को उन भावनाओं का अनुभव करने में सक्षम बनाती है।
3. ध्वनि सिद्धांत और रस
अभिनवगुप्त ने आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत (जिसे उन्होंने ध्वन्यालोक में विकसित किया) को रस सिद्धांत के साथ जोड़ा।
उन्होंने समझाया कि काव्य की ध्वनि और रस एक-दूसरे से कैसे जुड़े हैं।
उनके अनुसार, "ध्वनि" (suggestion) के माध्यम से रस का अनुभव गहराई से होता है।
4. दर्शक और अभिनेता का संबंध
अभिनवगुप्त ने बताया कि नाट्य का उद्देश्य दर्शकों को एक गहन अनुभव देना है।
अभिनेता और दर्शक के बीच एक भावात्मक और मानसिक जुड़ाव होता है, जिससे रस की अनुभूति होती है।
उन्होंने इस प्रक्रिया को एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में वर्णित किया।
5. नाट्यकला का उद्देश्य
अभिनवगुप्त ने नाट्य को केवल मनोरंजन का साधन न मानते हुए, इसे आत्मा के आनंद का माध्यम बताया।
उनके अनुसार, नाटक और काव्य का उद्देश्य आत्मा को उच्चतम आनंद (परमानंद) तक पहुँचाना है।
अभिनवभारती की शैली
तर्क और दर्शन का मिश्रण:
अभिनवभारती में अभिनवगुप्त ने तर्क और शैव दर्शन का उपयोग करके नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों को समझाया।
गूढ़ और सरलता का मेल:
उनकी शैली गहन दार्शनिक है, लेकिन विषय को इस तरह से प्रस्तुत करती है कि साधक या पाठक इसे समझ सके।
व्यवस्थित संरचना:
उन्होंने नाट्यशास्त्र के प्रत्येक अध्याय को अलग-अलग भागों में बाँटकर समझाया।
अभिनवभारती में शांत रस का महत्व
अभिनवगुप्त के अनुसार, शांत रस सभी रसों का मूल है।
यह रस आत्मा के अंतःसुख का प्रतीक है।
उन्होंने इसे शिव के आनंदस्वरूप से जोड़ा और बताया कि शांत रस के अनुभव से ही दर्शक और पाठक मुक्ति के मार्ग पर बढ़ सकते हैं।
अभिनवभारती का प्रभाव और महत्व
भारतीय सौंदर्यशास्त्र में योगदान:
अभिनवभारती भारतीय सौंदर्यशास्त्र की एक अनमोल धरोहर है।
यह ग्रंथ नाट्य और काव्य के सिद्धांतों को दर्शन और मनोविज्ञान से जोड़ता है।
नाट्यकला और साहित्य के अध्ययन में मार्गदर्शक:
इस ग्रंथ ने भारतीय और विश्व साहित्य में नाटक और कविता के अध्ययन की एक नई दृष्टि दी।
रस सिद्धांत का विस्तार:
रस सिद्धांत, विशेष रूप से शांत रस की व्याख्या, अभिनवभारती का सबसे बड़ा योगदान है।
शिवत्व की धारणा:
अभिनवगुप्त ने नाट्य और काव्य को शिव के आनंदस्वरूप से जोड़ा।
अभिनवभारती भारतीय काव्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र की गूढ़तम व्याख्याओं में से एक है। इसमें अभिनवगुप्त ने रस, नाट्य, काव्य, और दर्शक-अभिनेता के संबंध को गहराई से समझाया है। उनकी व्याख्या केवल सौंदर्यशास्त्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इन सभी तत्वों को दर्शन, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा गया है। यहाँ अभिनवभारती में निहित प्रमुख गूढ़ रहस्यों की व्याख्या दी गई है:
1. रस सिद्धांत का आध्यात्मिक रहस्य
भरत का सूत्र:
"विभावानुभावव्याभिचारि संयोगाद्रसनिष्पत्तिः"अभिनवगुप्त ने भरत के रस सिद्धांत को केवल नाटकीय आनंद तक सीमित न रखकर, इसे एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में देखा।
उन्होंने रस को "चेतना के विस्तार" के रूप में परिभाषित किया।
रस का अनुभव तभी होता है जब दर्शक अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को पीछे छोड़कर एक व्यापक सार्वभौमिक अनुभव में प्रवेश करता है।
रस और आत्मज्ञान:
रस को आत्मा की प्राकृतिक अवस्था के रूप में देखा गया।
सभी रस (श्रृंगार, वीर, करुण, आदि) एक उच्चतम अवस्था, शांत रस में विलीन हो जाते हैं।
शांत रस आत्मा का वह आनंद है जो ब्रह्म से एकाकार होने पर प्राप्त होता है।
2. साधारणीकरण (Universalization) का रहस्य
अभिनवगुप्त ने समझाया कि नाटक और काव्य में वर्णित भावनाएँ व्यक्तिगत नहीं रहतीं।
साधारणीकरण के माध्यम से, ये भावनाएँ सामान्य मानव अनुभव का हिस्सा बन जाती हैं।
यह प्रक्रिया दर्शकों को उनके स्वयं के "मैं" (ego) से मुक्त कर देती है और उन्हें एक सार्वभौमिक चेतना से जोड़ती है।
उदाहरण:
यदि नाटक में किसी पात्र की मृत्यु दिखाई जाती है, तो दर्शक केवल उस पात्र की मृत्यु को नहीं देखता, बल्कि जीवन और मृत्यु के व्यापक सत्य का अनुभव करता है।
3. शांत रस का सर्वोच्च स्थान
अभिनवगुप्त ने शांत रस को नौवाँ और सबसे महत्वपूर्ण रस माना।
यह सभी रसों का चरम और अंतिम लक्ष्य है।
शांत रस का अनुभव आत्मा की पूर्णता का प्रतीक है, जो शिव के आनंदस्वरूप से जुड़ा हुआ है।
उन्होंने शांत रस को "मुक्ति का माध्यम" बताया, क्योंकि यह आत्मा को जीवन और मृत्यु के बंधनों से परे ले जाता है।
4. नाट्य का दार्शनिक उद्देश्य
नाट्य केवल मनोरंजन नहीं है; यह आत्मा को जागृत करने का साधन है।
नाट्य कला "शिव की लीला" का प्रतीक है, जहाँ संसार एक नाटक के रूप में देखा जाता है।
अभिनवगुप्त ने नाटक को मायिक जगत (illusory world) से जोड़ा, जो वास्तविकता का प्रतिबिंब है।
नाटक में अभिनेता और दर्शक के बीच जो भावनात्मक संबंध बनता है, वह संसार के भीतर आत्मा और ब्रह्म के संबंध को दर्शाता है।
5. ध्वनि (Suggestion) का गूढ़ रहस्य
अभिनवगुप्त ने आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक सिद्धांत को रस सिद्धांत के साथ गहराई से जोड़ा।
ध्वनि (suggestion) काव्य या नाटक का सबसे शक्तिशाली तत्व है, जो सीधे दर्शक या पाठक की चेतना को प्रभावित करता है।
ध्वनि और रस का संबंध:
काव्य की ध्वनि पाठक या दर्शक को उसकी व्यक्तिगत भावनाओं से मुक्त कर एक सार्वभौमिक अनुभव की ओर ले जाती है।
उदाहरण: "चंद्रमा का वर्णन" केवल उसकी सुंदरता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि प्रेम, विरह, और शांति जैसे भावों का प्रतीक बन जाता है।
6. दर्शक और अभिनेता का गूढ़ संबंध
अभिनवगुप्त ने कहा कि नाटक तभी प्रभावी होता है जब दर्शक और अभिनेता के बीच "आध्यात्मिक सामंजस्य" स्थापित हो।
यह संबंध साधारणीकरण और रस सिद्धांत के माध्यम से बनता है।
दर्शक अपनी पहचान भूलकर अभिनेता के अनुभव को आत्मसात करता है।
यह प्रक्रिया "आत्मा के विस्तार" का प्रतीक है।
7. कला, काव्य, और धर्म का सामंजस्य
अभिनवगुप्त ने कला को धर्म और आध्यात्मिकता से जोड़ा।
नाटक और काव्य "धर्म" का एक माध्यम हैं, क्योंकि ये आत्मा को उच्चतम सत्य की ओर ले जाते हैं।
उन्होंने समझाया कि काव्य और नाटक में जो आनंद (रस) मिलता है, वह आत्मा के परमानंद (ultimate bliss) का प्रतीक है।
8. त्रिक दर्शन और रस सिद्धांत का संबंध
अभिनवगुप्त का त्रिक दर्शन (कश्मीर शैव दर्शन) अभिनवभारती की गहराई को बढ़ाता है।
उन्होंने शिव, शक्ति, और आत्मा के संबंध को नाटक और रस के अनुभव में जोड़ा।
नाटक में:
शिव: नाटक का आधार या चेतना।
शक्ति: नाटक की गतिविधि या कथा।
आत्मा: दर्शक का अनुभव, जो शिव और शक्ति के मिलन से उत्पन्न होता है।
9. काव्य में नैतिकता और मानवता का स्थान
काव्य और नाटक का उद्देश्य केवल आनंद नहीं है, बल्कि मानवता को एक उच्चतर नैतिक और आध्यात्मिक अवस्था तक पहुँचाना है।
अभिनवगुप्त ने कहा कि नाटक और काव्य में "धर्म" और "मानवता" के संदेश छिपे होते हैं, जिन्हें दर्शक और पाठक अनुभव करते हैं।
10. शिव और नाटक का संबंध
अभिनवगुप्त ने नाटक को शिव के नृत्य (तांडव) से जोड़ा।
शिव का नृत्य ब्रह्मांडीय सृष्टि, स्थिति, और संहार का प्रतीक है।
नाटक में पात्रों और कथाओं के माध्यम से यही सृष्टि, स्थिति, और संहार दिखाई देता है।
उन्होंने कहा कि नाटक और काव्य के माध्यम से व्यक्ति "शिव के खेल" को समझ सकता है।
अभिनवभारती के गूढ़ रहस्यों का सार
कला और दर्शन का मिलन:
काव्य और नाटक केवल कला नहीं हैं; ये आत्मा की मुक्ति का साधन हैं।
शांत रस की प्रधानता:
शांत रस आत्मा का सर्वोच्च आनंद है, जो आत्मज्ञान और मुक्ति का द्वार खोलता है।
दर्शक की चेतना का जागरण:
नाटक और काव्य के माध्यम से दर्शक अपनी चेतना का विस्तार कर सकता है।
सार्वभौमिक अनुभव का महत्व:
काव्य और नाटक का उद्देश्य व्यक्तिगत भावनाओं को सार्वभौमिक बनाना है।
त्रिक दर्शन का समावेश:
शिव और शक्ति की अवधारणा के माध्यम से, नाट्य और काव्य को ब्रह्मांडीय सत्य से जोड़ा गया है।
अभिनवभारती केवल रस और नाट्य सिद्धांत का ग्रंथ नहीं है; यह भारतीय दर्शन, काव्यशास्त्र, और सौंदर्यशास्त्र का एक महान समन्वय है। इसमें निहित गूढ़ रहस्य यह बताते हैं कि नाट्य और काव्य केवल आनंद प्रदान करने का साधन नहीं हैं, बल्कि आत्मा को उसकी उच्चतम अवस्था तक ले जाने का मार्ग भी हैं। अभिनवगुप्त ने इसे आध्यात्मिकता, दर्शन, और कला के संगम के रूप में प्रस्तुत किया, जो हर युग में प्रासंगिक रहेगा।
हमारा उद्देश्य केवल सजगता बढ़ाना है ,हम जन साधारण को संतो, ध्यान विधियों ,ध्यान साधना से संबन्धित पुस्तकों के बारे मे जानकारी , इंटरनेट पर मौजूद सामग्री से जुटाते है । हम किसी धर्म ,संप्रदाय ,जाति , कुल ,या व्यक्ति विशेष की मान मर्यादा को ठेस नही पहुंचाते है । फिर भी जाने अनजाने , यदि किसी को कुछ सामग्री सही प्रतीत नही होती है , कृपया हमें सूचित करें । हम उस जानकारी को हटा देंगे ।
website पर संतो ,ध्यान विधियों , पुस्तकों के बारे मे केवल जानकारी दी गई है , यदि साधकों /पाठकों को ज्यादा जानना है ,तब संबन्धित संस्था ,संस्थान या किताब के लेखक से सम्पर्क करे ।
© 2024. All rights reserved.